साल 1967 में छह दिनों तक चले फ़लस्तीन युद्ध, उसमें तीन अरब देशों की हार और उन देशों के हिस्सों पर इज़रायल के क़ब्जे ने पूरे मध्य-पूर्व की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी।
यहूदियों-मुसलमानों के पवित्र शहर पूर्वी येरूशलम पर इज़रायल के कब़्जे ने इज़रायल-फ़लस्तीन विवाद को भी बदल दिया और इस विवाद के दोनों पक्षों को भी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर किया।
इज़रायलियों में अंध राष्ट्रवाद की भावना भरने लगी तो फ़लस्तीनियों में भी एक नए किस्म का राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। यह राष्ट्रवाद सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि पहचान से जुड़ा हुआ था।
अरब राष्ट्रवाद
यह अरब राष्ट्रवाद था, फ़लस्तीनी पहचान की लड़ाई थी। इस लड़ाई को इन देशों के शासकों की निजी कोशिशों, रणनीतियों और लाभ-हानि से बाहर निकाल कर आम जनता से जोड़ने की मुहिम शुरू हुई।
इसमें आम जनता की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सरकार के फ़ैसलों का समर्थन करने के बजाय ख़ुद फ़ैसले लेने वाले के रूप में स्थापित करने की कोशिशें शुरू हुईं।
फ़लस्तीन मुक्ति मोर्चा यानी पीएलओ और पॉपुलर फ्रंट फ़ॉर लिबरेशन ऑफ़ पैलेस्टाइन जैसे संगठन इस मक़सद से ही बनाए गए कि इस आन्दोलन में आम जनता की भागीदारी हो, फ़लस्तीनी अपनी लड़ाई खुद लड़ें, वे इसके लिए सड़कों पर उतरें। पीएलओ की स्थापना 1964 में हुई और 1969 में यासर अरफ़ात इसके नेता चुने गए।

यासर अरफ़ात तेज़-तर्रार, अच्छे वक्ता और संगठन बनाने व लोगों को जोड़ने में कुशल थे। जल्द ही पीएलओ का आधार गज़ा पट्टी और पश्चिमी तट पर बढ़ता गया। इसे अरब लीग ने मान्यता दे दी और वह उसका सदस्य भी बन गया। इसने अपना मुख्यालय जोर्डन में बनाया क्योंकि पश्चिमी तट व गज़ा पट्टी में इज़रायल इसे काम नहीं करने दे सकता था।
पीएलओ
साल 1969 के निर्णायक युद्ध और उसमें जोर्डन की हार का नतीजा यह निकला कि 1970 में इसे जोर्डन छोड़ कर लेबनान में शरण लेनी पड़ी। पीएलओ इज़रायली सुरक्षा बलों पर लेबनान से पलटवार किया करता था। इज़रायल ने लेबनान पर 1982 में हमला कर दिया और उसकी राजधानी बेरूत पर कब्जा कर लिया। पीएलओ को लेबनान छोड़ना पड़ा और उसने ट्यूनिशिया में शरण ली।
शांति प्रक्रिया
इज़रायल ने पीएलओ को मान्यता नहीं दी थी और उसे फ़लस्तीनियों का प्रतिनिधि नहीं मानता था। जिमी कार्टर ने 1977 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद मध्य-पूर्व शांति वार्ता की कोशिशें शुरू कीं। अमेरिकी विदेश मंत्री साइरस वान्स ने इज़रायल, मिस्र, सीरिया और जोर्डन से गोपनीय बात शुरू की।
लगभग सवा साल की बातचीत के बाद अमेरिकी राज्य मेरीलैड के कैंप डेविड नामक जगह पर खुली बातचीत हुई और इन देशों के प्रमुख खुल कर सामने आए।
कैंप डेविड समझौता
कैंप डेविड समझौते पर इज़रायली प्रधानमंत्री मेनाहिम बेगिन, मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात, सीरिया के हाफिज़ अल असद और जोर्डन के शाह हुसैन ने 17 सितंबर, 1978 को दस्तख़त किए। इस समझौते में पहली बार फ़लस्तीनियों के आत्म निर्णय के अधिकार को स्वीकार किया गया।

- यह तय हुआ कि पश्चिमी तट और गज़ा पट्टी से इज़रायली सेना वापस चली जाएगी।
- पश्चिमी तट के लिए अलग से पुलिस बल बनाया जाएगा जिसमें जोर्डन के नागरिक होंगे।
- जोर्डन और इज़रायल की संयुक्त टीम पश्चिमी तट की निगरानी करेगी।
- पश्चिमी तट और गज़ा पट्टी में स्थानीय प्रशासन के निकाय बनाए जाएंगे, आम जनता इसके प्रतिनिधियों को चुनेगी।
- इन निकायों को स्व-शासन के सारे अधिकार सौंप दिए जाएंगे।
- ये दोनों ही इलाक़े स्वायत्त होंगे और इन पर इज़रायल का नियंत्रण नहीं होगा। यह सारा काम पाँच साल में पूरा कर लिया जाएगा।
इज़रायल को मिली मान्यता
इस समझौते में मिस्र, सीरिया और जोर्डन ने आधिकारिक रूप से इज़रायल को मान्यता दे दी और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। इन देशों के साथ इज़रायल के कूटनीतिक रिश्ते बन गए और अंतरराष्ट्रीय जगत में इज़रायल के प्रति लोगों का रवैया थोड़ा नरम हुआ।
मेनाहिम बेगिन और अनवर सादात को कैंप डेविड समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। लेकिन 1981 में सादात की हत्या कर दी गई। इज़रायल में इस समझौते की तीखी आलोचना हुई और मेनाहिम बेगिन की राजनीति ख़त्म हो गई, वह अगला चुनाव हार गए।
संयुक्त राष्ट्र ने कैंप डेविड समझौते को खारिज कर दिया। इसकी वजह यह थी कि इसमें स्वतंत्र फ़लस्तीन देश की कोई चर्चा नहीं थी, शरणार्थियों की वापसी और पूर्व येरूशलम पर कुछ नहीं कहा गया था, इसमें किसी फ़लस्तीनी संगठन को नहीं बुलाया गया था।
अगला समझौता
इस समझौते से पीएलओ को यह फ़ायदा हुआ कि यह मान लिया गया कि उसके बग़ैर किसी समझौते का कोई अर्थ नहीं है। मध्य-पूर्व में शांति बहाली करनी है तो पीएलओ को लेकर चलना होगा।
बिल क्लिंटन ने जनवरी 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद 1993 में मध्य-पूर्व शांति समझौते की कोशिशें शुरू कीं क्योंकि कैंप डेविड समझौता पिट चुका था, इस समस्या के मौलिक मुद्दे ही गौण रह गए थे।
ओस्लो शांति क़रार
पूर्व येरूशलम की स्थिति, शरणाथियों की वापसी, गज़ा पट्टी व पश्चिमी तट के प्रशासन की स्थिति, इज़रायल सैनिकों की वापसी और इज़रायल व फ़लस्तीन की सीमा तय नहीं हुई थी। इसलिए क्लिंटन ने ठीक इन्हीं मुद्दों पर बात शुरू की और जहाँ कैंप डेविड समझौता ख़त्म हुआ था, वहीं से अगले समझौते की शुरूआत की गई।
इस समझौते के दो चरण थे यानी दो अलग-अलग क़रारों पर हस्ताक्षर किए गए, एक बार 1993 में और दूसरी बार 1995 में। पहली बार के क़रार में फ्रेमवर्क तय हुआ था, यानी किन मुद्दों पर बात होनी है, यह तय हुआ था और दूसरी बार यानी 1995 में समझौते पर दस्तख़त हुए थे। इस पूरी प्रक्रिया को ओस्लो शांति समझौता 1993 ही कहते हैं।
नॉर्वे के शहर ओस्लो में पीएलओ के लोग और इज़रायल सरकार के वार्ताकार एकत्रित हुए और अमेरिकी मध्यस्थता में बातचीत शुरू हुई, पर यह पूरी तरह गोपनीय थी।

अमेरिकी शहर वाशिंगटन में सितंबर में इज़रायली सरकार और पीएलओ के लोगों ने खुले आम बातचीत की।
इज़रायली प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन और पीएलओ के अध्यक्ष यासर अरफ़ात ने 28 सितंबर 1995 को इस पर दस्तख़त किए।
इस समझौते की अहम बातें थीं-
- पीएलओ ने इज़रायल राज्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, इज़रायलियों के जीने के हक़ को स्वीकार किया और आतंकवाद व हर तरह की हिंसा छोड़ने का एलान किया।
- इज़रायल ने पीएलओ को फ़लस्तीनियों का प्रतिनिधि मान लिया।
- यह तय हुआ कि पश्चिमी तट व गज़ा पट्टी से इज़रायली सैनिक हटा लिए जाएंगे।
- गज़ा पट्टी व पश्चिमी तट में फ़लस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकार यानी पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी का गठन किया जाएगा।
- इसके प्रतिनिधि आम जनता से चुने जाएंगे।
- इसके पास किसी भी सरकार की तरह हर तरह के विधायी, प्रशासकीय व राजनीतिक अधिकार होंगे।
- इसकी अपनी पुलिस होगी।
फ़लस्तीन देश नहीं!
लेकिन इस क़रार में भी अलग फ़लस्तीन राज्य की बात नहीं थी। यानी फ़लस्तीन के पास सबकुछ होगा, पर सार्वभौमिक अधिकार नहीं होगें, वह एक अलग देश नहीं होगा।
इज़रालय में इस शांति समझौते का विरोध एक बार फिर कट्टर राष्ट्रवादियों ने किया, जिनकी नज़र में यह यहूदी राज्य के प्रति विश्वासघात था। नवंबर 1995 में यित्ज़ाक राबिन की हत्या एक कट्टर यहूदी ने कर दी।
राबिन के बाद शिमोन पेरेस प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लोगों के विरोध के बावजूद समझौते को माना और उसे लागू करने की बात दुहराई।
लेकिन 1996 के आम चुनाव में शिमोन पेरेस की पार्टी हार गई, लिकुड पार्टी ने जीत दर्ज की और बिन्यामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री चुने गए।
समझौते पर सवाल
नेतन्याहू ने कामकाज संभालते ही समझौते पर सवाल उठाना और उसे लागू करने में अड़ंगा डालना शुरू किया।
बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि समझौते को एक बार में ही लागू न कर टुकड़ों में लागू किया जाए यानी पहले एक बात लागू हो, उसका नतीजा देखा जाए, फिर अगली शर्त लागू हो।
वाई रिवर मेमोरंडम
बिल क्लिंटन ने एक बार फिर इज़रायल पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अंत में काफी दबाव व मान मनौव्वल के बाद अक्टूबर, 1998 में अमेरिका के मेरीलैंड में वाई रिवर मेमोरंडम पर दस्तख़त किए गए। यासर अरफ़ात और बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस पर दस्तख़त किए।
इस क़रार में नया कुछ नहीं था, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू ने औपचारिक रूप से यह आश्वासन दिया कि वह ओस्लो शांति समझौते को लागू करेगा। उन्होंने इसे इज़रायली संसद से पारित भी करवा लिया। यानी पहली बार इज़रायली संसद ने फ़लस्तीनियों के अधिकारों को स्वीकार किया।

पैलेस्टाइन अथॉरिटी के पास राजनीतिक, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय अधिकार थे, लेकिन अभी भी पश्चिमी तट कई टुकड़ों में बँटा हुआ था, उसके 60 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर इज़रायल का शासन था, इज़रायली सैनिक तो थे ही।
कैंप डेविड समझौता 2000
एक बार फिर बातचीत शुरू हूई। अंत में साल 2000 में एक दूसरा कैंप डेविड समझौता हुआ, जिस पर इज़रायली प्रधानमंत्री एहुद बराक़ और यासर अरफ़ात ने दस्तख़त किए।
पहली बार इज़रायल ने अपनी सेना पूरे फ़लस्तीनी इलाक़े से हटा ली। पैलेस्टाइन अथॉरिटी के पास पूरा इलाक़ा कब्जे मे आ गया।

टूटा हुआ ख्वाब!
लेकिन फ़लस्तीन के दुख का अंत नहीं हुआ है। फ़लस्तीन अभी भी अलग स्वतंत्र देश नहीं बना है। उस पर सीधा इज़राइली शासन नहीं है, वह स्वायत्त क्षेत्र है।
बिन्यामिन नेतन्याहू ने 2005 में अतंकवादी हमले रोकने के नाम पर इज़रायल के चारों ओर ऊँची दीवार बनवानी शुरू कर दी, वह बन चुकी है। लेकिन वह दीवार फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर बनी है।
आज भी गज़ा पट्टी व पश्चिमी तट अलग-अलग हिस्सों में हैं, उनके बीच इज़रायल है। एक इलाक़े से दूसरे इलाक़े में जाने के लिए कई चेक प्वाइंट को पार करना पड़ता है, फलस्तीनियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है।
इज़रायल अभी भी ज़मीन हड़पने में लगा हुआ है। वह पश्चिमी तट के नए- नए इलाक़ों में यहूदियों की बस्तियाँ बनवा रहा है। वह फ़लस्तीनियों को खदेड़ने और चेक प्वाइंट्स से उनका जीवन दूभर करने में लगा हुआ है।
अरफ़ात पर भी उठे थे सवाल
यहूदियों को अपनों से भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं मिला। विदेशों से मिले करोड़ों डॉलर फ़लस्तीनियों पर नहीं खर्च कर निजी जिंदगी पर खर्च करने का आरोप यासर अरफ़ात पर लगा था।
उनकी पत्नी सूहा शाह खर्च थीं, जिससे खुद फ़लस्तीनी प्रशासन के लोग परेशान थे, हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी से पैसे नहीं लिए थे।

महमूद अब्बास की आलोचना
अरफ़ात ने ही महमूद अब्बास को पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी का अध्यक्ष बनवाया था, पर सारे अधिकार अपने पास रखे थे। अब्बास से उनकी नहीं बनती थी।
नवंबर, 2004 से आज तक पीएनए के अध्यक्ष महमूद अब्बास ही हैं। उन्होंने किसी दूसरे नेता को पनपने नहीं दिया, चुनाव नहीं करवाए। सएब एराकात और हैनन अशरवी जैसे तेज़ तर्रार नेता पूरी तरह उपेक्षित रह गए। लेकिन आज खुद अब्बास पूरी तरह हाशिए पर हैं।

ख़्वाब जो आज भी अधूरा है!
साल 2007 के चुनाव में पश्चिमी तट उनके हाथ से निकल गया, उस पर हमास का कब्जा हो गया। हमास के लड़ाकों ने अब्बास की पार्टी फ़तह के लोगों को पश्चिमी तट से बाहर कर दिया है।
पश्चिमी तट की बागडोर इसमाइल हानिया के हाथों में हैं। अब वे ही फलस्तीनियों के नेता माने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिलने के बावजूद उनकी उपेक्षा मुश्किल है।
फ़लस्तीन आज भी बंटा हुआ है, टुकड़ों में है। आज भी फ़लस्तीन देश नहीं बना है। बालफोर डेक्लेरेशन के सौ साल हो चुके हैं, इज़रायल तो बन गया, पर फलस्तीन आज भी नहीं बना है।
पूर्वी येरूशलम अभी भी इज़रायलियों के कब्जे में है। शरणार्थियों की तीसरी पीढी शरणार्थी शिविरों में ही रह रही हैं। उनकी संख्या अब लाखों में हो चुकी है।
बालफोर डेक्लेरेशन अधूरा है। मृत सागर यानी डेड सी वाकई मृत पड़ा हुआ है। उसे फ़लस्तीनियों की कोई सुध नहीं है।

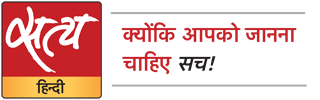





















अपनी राय बतायें