दिल्ली के आसपास के शहरों में कमाई के अवसर शून्य हो जाने के बाद गाँव की तरफ़ पैदल जाने वालों का रेला इंसानियत को चुनौती दे रहा है। इतनी लम्बी दूरी पैदल तय करने की योजना बनाना इस बात का साफ़ सबूत है कि दिल्ली में रहना असंभव हो गया है। लेकिन इसके पीछे शहरों की तरफ़ भगदड़ सबसे बड़ा कारण है। जो लोग जा रहे हैं लगभग उन सब की गाँव में अपनी ज़मीन है जिसमें गुज़र-बसर हो सकता है। लेकिन वे शहर में बेहतर ज़िंदगी के सपने देखकर यहाँ आए थे।
मैंने इन सपनों के निर्माण की फ़र्ज़ी प्रक्रिया को बहुत क़रीब से देखा है। उत्तर प्रदेश के गाँवों में रहने वाले लड़कों के मन में शहरों की ज़िंदगी की एक तसवीर रहती है। लेकिन सचाई कुछ अलग होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। गाँव में रहते हुए बड़े शहरों की ज़िंदगी के बारे में सम्पन्नता की कल्पना हावी रहती है। मेरा यह सपना बहुत जल्दी टूट गया था लेकिन सबको यह अवसर नहीं मिलता। मैं पहली बार जब दिल्ली आया तो दिमाग़ में एक पता बहुत साफ़ लिखा हुआ था- गली मैगज़ीन, चूड़ी वालान, चावड़ी बाज़ार, चांदनी चौक, दिल्ली। मेरे गाँव के कुछ लोग यहाँ रहते थे।
जब वे लोग गाँव जाते थे तो सबसे बढ़िया धोती, बढ़िया कुर्ता, गले में महकता हुआ पाउडर लगा हुआ होता था। किसी की शादी में द्वारपूजा के लिए जब आते थे तो सबसे प्रभावशाली लगते थे। बिरला के बैंक यूनाइटेड कमर्शियल में काम करते थे। जब मई-जून में गाँव आते थे तो लगता था कि उनके पास बहुत पैसा है। मैं सोचता था कि सम्पन्नता तो दिल्ली में ही कमाने से आती है। उसी दौर में जौनपुर अपने मामा के गाँव गया। वहाँ किसी पड़ोसी के कोई रिश्तेदार भीखाभाई की चाल, अहमदाबाद में रहते थे। उनके भी कपड़े, साबुन, सिगरेट वगैरह माहौल में ख़ुशबू बिखेरते थे।
1967 में मैं अपनी बहन के यहाँ गया। वहाँ कोई रिश्तेदार आए हुए थे, वे सलाबतपुरा, बेग़म बाड़ी सूरत में रहते थे। उनके कपड़े बहुत ही साफ़-सुथरे होते थे। महँगी घड़ी, क़लम आदि उनके पास भी होती थी। मन में कहीं बैठ गया कि सम्पन्नता इन्हीं शहरों में है।
बंबई के बारे में ऐसे रूमानी ख़याल नहीं थे क्योंकि मेरे ख़ानदान के मेरे पिताजी से उम्र में बड़े ठाकुर रामबक्स सिंह मुंबई में रहते थे, देना बैंक में काम करते थे और बंबई के बारे में बहुत रोमांटिक तसवीर नहीं पेश करते थे। कहते थे कि पैसा तो बंबई में मिलता है, महाजनी नौकरी में पगार ईमानदारी से पूरी मिलती है लेकिन ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। रहने और संडास जाने की बहुत तकलीफ होती है।
शहर का सपना टूटा
अवध के सुल्तानपुर ज़िले में रहने वाले एक किशोरवय लड़के के सपने यानी मेरे सपने जल्दी टूट गए। 1971 में जब मैंने बीस साल की उम्र में दिल्ली की पहली यात्रा की तो गली मैगज़ीन, चूड़ी वालान, चावड़ी बाज़ार, चांदनी चौक जाने का मौक़ा मिला। देखा तो वह एक बहुत ही गंदी गली थी। इतवार का दिन था। मेरे गाँव के जो श्रीमानजी वहाँ रहते थे वे दूसरी मंजिल पर एक कोठरी में रहते थे। पटरे के जांघिया पहने बैठे थे, उनके छोटे भाई नहीं दिखे। मैंने पूछा तो बताया कि अभी आ रहे हैं। पानी लेने गए हैं। मैं भी नीचे चला गया। एक सरकारी नल था, वहीं कई लोग पानी लेने के लिए लाइन में लगे थे। बहरहाल, जब वहाँ से लौटकर आया तो समझ में आ चुका था कि दिल्ली की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है।
उन दोनों भाइयों के कपड़ों की तुलना में उनकी मलिन बस्ती की ज़िंदगी बार-बार यादों में घूमती रही। अहमदाबाद या सूरत वालों के यहाँ तो कभी नहीं गया लेकिन समझ में आ गया कि गाँव आने की तैयारी में परदेसिहा ख़ास तौर से कपड़े खरीदता है।
मैं तो भाग्यशाली था, समझ में बात आ गयी लेकिन बहुत सारे लड़कों के दिमाग़ में यह तसवीर बनी रहती है। गाँव में मेहनत करते रोटी कमाने को मुसीबत मानने वाले बाभन-ठाकुर के लड़के महानगर में जाना चाहते हैं और हाई स्कूल या इंटर पास करके चले आते हैं। जिसके यहाँ आकर रहते हैं दो-चार दिन बाद ही वह कहने लगता है कि भाई अपनी खोराकी तो कमाओ और उनको किसी भी मज़दूरी की लाइन में खड़े होना पड़ता है, किसी लेबर चौक पर खड़े होकर दिन की मज़दूरी का इंतज़ार करना पड़ता है। और किसी तरह रोज़ की रोटी कमाने लगते हैं। जब गाँव वापस जाते हैं तो किसी को सच्चाई नहीं बताते। सच्चाई यह है कि इतनी मेहनत करके दिल्ली में दो जून की रोटी कमाते हैं अगर उतनी मेहनत अपने गाँव के खेत में करें तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़ुशनुमा होगी लेकिन ऐसा वे नहीं करते। एकाध साल बाद अपनी पत्नी को ले आते हैं और महानगर की ज़िंदगी में किसी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला एक परिवार जुड़ जाता है। बाद में वही लोग पूर्वांचली वोट बैंक का हिस्सा बन जाते हैं।
चुनाव के पहले कुछ मलिन बस्तियों को पानी-बिजली के कनेक्शन मिलते हैं और लोग दिल्ली शहर में मकान मालिक बन जाते हैं। जब वे लोग गाँव जाते हैं तो सम्पन्नता की मूर्ति लगते हैं। उनकी जीवनशैली गाँव में एकदम अलग होती है लेकिन शहर में वे किसी संगम विहार, किसी सोनिया विहार या किसी मंडावली में अपनी बस्ती के रेगुलर होने के इंतज़ार में उम्र बिता देते हैं। गाँव में जाकर सच्चाई नहीं बताते।
सच्चाई छुपाने का नतीजा यह होता है कि शहर की तरफ़ अगली खेप आ जाती है। दो-चार साल सड़क या किसी नाली के किनारे ज़िंदगी बिताने के बाद वे भी कहीं किसी प्रॉपर्टी माफिया के शिकार होते हैं और क़र्ज़ आदि लेकर पचीस से पचास गज के बीच की ज़मीन किसी कच्ची कॉलोनी में ख़रीद कर घर बना लेते हैं। फिर वही शहर की गंदी बस्ती की ज़िंदगी, वही वोट बैंक, वही सपन्नता का ढोंग और वही नए लड़कों के दिल्ली आने का दुश्चक्र फिर खेला जाता है।
पैदल जा रही भीड़ में वही लोग हैं जिनकी जाति ऐसी है जो गाँव में मनरेगा में मज़दूरी नहीं कर सकते। लगभग सभी तथाकथित ऊँची जाति के हैं। हज़ारों मील पैदल जाना तो शायद नहीं हो पाएगा, सरकार उन लोगों को कभी न कभी गंतव्य तक पहुँचा देगी। लेकिन अगर वे जितनी मेहनत यहाँ दो जून की रोटी के लिए कर रहे थे अपने गाँव में रुककर ही उसकी आधी मेहनत भी करेंगे तो गाँव में इससे बेहतर ज़िंदगी जिएँगे। अपने पुरखों की ज़मीन का सम्मान करेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ छोड़कर जाएँगे।










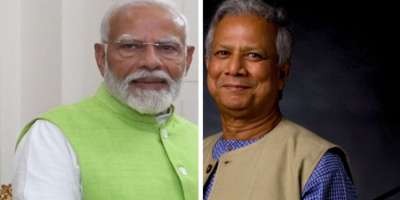























अपनी राय बतायें