दिसम्बर के आख़िरी हफ्ते में किसी दिन फोन पर आवाज आईः ‘सर, मैं रोहिण कुमार हूं—लाल चौक नाम से कश्मीर पर एक किताब लिखी है। आपको भेजना चाहता हूँ। आपका डाक-पता चाहिए था।’ उस समय तक मेरी रोहिण से कभी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी इस किताब के बारे में मैं देख-सुन चुका था।
कश्मीर मामलों पर लिखने-पढ़ने के चलते इस किताब में मेरी भी रूचि थी कि आख़िर एक युवा-पत्रकार ने अपनी किताब में क्या कुछ लिखा है! रोहिण ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह न्यूजलॉन्ड्री और कुछ अन्य वेबसाइटों के लिए काम कर चुका है। जिन मीडिया संस्थाओं का उसने नाम लिया, वे पत्रकारिता को गंभीरता से लेती हैं, इसलिए रोहिण के पत्रकार होने पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता था। मैंने फ़ौरन उन्हें अपना पता भेजा। हालचाल भी लिया-कहां के रहने वाले हैं? उन्होंने बताया-‘बिहार के गया से हूँ।’
अब रोहिण की किताब मैं पढ़ चुका हूँ। बिहार से आकर दिल्ली में काम कर रहे इस युवा पत्रकार ने कश्मीर पर लिखने का अच्छा और ईमानदार प्रयास किया है। इसके लिए उसने पहले की छपी किताबों या आलेखों का सहारा भर नहीं लिया है। वह घाटी के दहकते और सुबकते चिनारों से लगातार रू-ब-रू हुआ है। उनसे संवाद किया है। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, छोटे-मझोले कस्बों और यहाँ तक कि गांवों का भी दौरा किया है।
256 पृष्ठों की किताब में सिर्फ़ समझ और साहस ही नहीं, लेखक की मेहनत भी दिखती है, जो सामाजिक-आर्थिक विषय पर लिखने वाले हिन्दी के अधिसंख्य लेखकों-पत्रकारों में ज़्यादा नहीं दिखती। यह कश्मीर के समकालीन इतिहास पर सिर्फ सूचना देने वाली किताब नहीं है, मौजूदा परिदृश्य की जटिलताओं और उलझावों से जूझने वाला दस्तावेज भी है। यह ‘कट-एंड-पेस्ट’ वाला उपक्रम नहीं है, जैसा अंग्रेजी की कई किताबों में दिखता रहा है। हिन्दी में तो वैसे भी कश्मीर पर बहुत कम किताबें हैं।
कश्मीर को लेकर अपने ज्ञान के लिए सिर्फ़ हिन्दी-अंग्रेजी के न्यूज चैनलों या हिन्दी अख़बारों पर निर्भर रहने वाले कुछ हिन्दी साहित्यकारों, एंकरों और शिक्षकों ने पिछले दिनों कश्मीर पर छपी एक किताब-‘कश्मीरनामा’ की काफी चर्चा की थी। उसे कश्मीर पर लिखी ‘हिन्दी की पहली मुकम्मल किताब’ बताया गया था। उस किताब को मैं शुरू से आख़िर तक पढ़ गया और ‘प्रतिमान’ में उस पर लिखा भी। आम जानकारी के हिसाब से वह पाठ्यक्रम की किसी स्थूलकाय किताब की तरह उपयोगी है। उसमें कश्मीर के इतिहास के ज़रूरी विवरण हैं पर आज का कश्मीर नहीं है, उसकी अवाम, उसके मसले और उसकी जद्दोजहद नहीं है। उससे समकालीन कश्मीर पर कोई स्पष्ट दृष्टि या समझ नहीं उभरती। लेखक ने उस किताब के आख़िर में (पृष्ठ-432) कश्मीर मसले के समाधान के रास्ते का उल्लेख किया है और वह दो तरह के विकल्पों की बात करता है-डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और डायलॉग।
दूसरा ‘दुर्भाग्यपूर्ण विकल्प’ ‘डिफ़ेंस’ के इस्तेमाल को बताया गया है! मतलब मिलिट्री आप्शन! किताब के आखिर में उल्लिखित ये आखिरी विकल्प किताब के पूरे कश्मीर-विमर्श को संदिग्ध बना देता है।
पत्रकार रोहिण कुमार की किताब इस माय़ने में बिल्कुल अलग परम्परा की किताब है। वह ऐसे किसी विकल्प को शुरू से आखिर तक खारिज करती है। वह एक पत्रकार के श्रम, शोध और समझ का नतीजा है।
प्रस्तावना में लेखक का यह कहना महज कागजी दावा नहीं है कि उसने कश्मीरियों के ‘फर्स्ट हैंड नैरेटिव’ को किताब में तवज्जो दी है, किताब को जो भी पढ़ेगा, उसे यह एक ईमानदार बयान लगेगा।
‘लाल चौक’ (वर्ष-2021, प्रकाशकः हिंद युग्म, सेक्टर-20, नोएडा, यूपी) जैसी किताब ढेर सारी किताबों को पढ़कर नहीं लिखी जा सकती। इसके लिए विषय से टकराना होता है, विषय के भूगोल, इतिहास और उसके अलग-अलग किरदारों से रू-ब-रू होना होता है। घटनाओं की तह में जाकर पड़ताल करनी होती है। रोहिण इसके लिए कश्मीर घाटी के बहुत सारे इलाक़ों और बहुत तरह के लोगों से रू-ब-रू हुए हैं। उनकी किताब पढ़ते हुए यह कोई भी महसूस कर सकता है। बहुत सारे लोगों और घटनाओं से रू-ब-रू होने और तथ्यों की पड़ताल के बाद कश्मीर पर लेखक की जो धारणा या विचार उभरकर सामने आये हैं, उनसे किसी का सहमत या असहमत होना स्वाभाविक है। पर उऩकी पड़ताल के मौलिक और प्रामाणिक होने के तथ्य को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
लेखक ने साहस के साथ कश्मीर के सच को लिखने की कोशिश की है।
इस कोशिश में उनकी कुछ कमियां या कमजोरियां भी गिनाई जा सकती हैं। मुझे जो कुछ कमियां नज़र आईं, उनमें एक है- सरहदी सूबे में कश्मीरियों के अलगाव के कारणों में उनकी अपनी भूमिका को नजरअंदाज़ करना। लेखक ने लद्दाख और जम्मू के कुछ प्रतिनिधियों के भी इंटरव्यू छापे हैं पर कश्मीरियों के जम्मू और लद्दाख वालों से बनती दूरी, अलगाव और संवादहीनता की वजहों पर इस किताब में बहुत कम चर्चा है। कश्मीरी अवाम के दुख-दर्द में उनके साथ गहरी सहानुभूति जताना ग़लत नहीं है। पर कश्मीरियों के राजनीतिक नेतृत्व के बौद्धिक और वैचारिक दिवालियेपन पर बातचीत करना आज ज़रूरी है। कश्मीर के संदर्भ में आज का यह एक बड़ा प्रश्न है। इस बात की पड़ताल होनी चाहिए कि नेतृत्व के बौनेपन की वजह क्या है?
बीते तीन दशकों के दौरान अविभाजित सरहदी सूबे के विभिन्न इलाक़ों और समाजों की कुछ न्यूनतम मुद्दों पर भी एकजुटता क्यों नहीं हो सकी? विभाजन और अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान वाले हिस्से के निरस्त किये जाने के बाद आज जम्मू और लद्दाख में भी कश्मीर घाटी की तरह अपनी ज़मीन-जायदाद और विशिष्ट पहचान के संरक्षण के सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी के राजनीतिक-प्रभाव वाले लद्दाख में इस मुद्दे पर ‘बंद’ आयोजित किया गया था। देश की अन्य लोकतांत्रिक शक्तियों और कश्मीरी नेतृत्व के बीच लगभग संवादहीनता रही है।
क्या कश्मीर मसले के अंतरराष्ट्रीयकरण पर ज्यादा जोर देने के चलते घरेलू स्तर पर कश्मीरियों, खासकर कश्मीरी राजनीति में मुख्यधारा के संगठन कह जाने वालों ने देश के अंदर अपने संभावित समर्थन के दायरे को बढ़ जाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया?
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आखिरी नेता थे, जिन्होंने देश की घरेलू राजनीति में अपने लिए समर्थन जुटाने की क्षमता अर्जित की थी। उनके लिए जयप्रकाश नारायण सरीखे वाम से दक्षिण की तरफ़ झुके पूर्व समाजवादी, कई मध्यमार्गी और अनेक वामपंथी भी आवाज़ उठाते थे।
एक विनम्र सुझाव और। करगिल को हर जगह कारगिल लिखना अटपटा है। इसी तरह शेख मो. अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला को अब्दुल्लाह क्यों? हिन्दी में सभी अब्दुल्ला ही लिखते हैं।
‘लाल चौक’ में समकालीन कश्मीरी समाज की रिपोर्टिंग-आधारित जो तसवीर पेश की गयी है, वह इस किताब की जान है। अतीत के महत्वपूर्ण प्रसंगों के ब्योरों में कई जगह आधी-अधूरी बातें हैं। शायद, संक्षिप्त होने के दबाव में। किताब के पहले अध्यायः ‘अपना-अपना सच--’ में कई जगह यह कमी खलती है। सन् 1950 के भूमि-सुधार के बड़े क़दम की चर्चा तो है पर सन् 1953 के अगस्त महीने में सूबे के वजीरे आजम शेख अब्दुल्ला के पद से हटाने के साथ ही गिरफ्तारी के प्रसंग में कई ज़रूरी तथ्य नजरअंदाज़ हो गये हैं।




















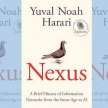















अपनी राय बतायें