नए भारत में आज़ादी एक बदनाम शब्द है। नहीं, बदनाम से भी ज़्यादा यह एक ख़ौफ़नाक़ शब्द बन चुका है। इस शब्द के इस्तेमाल की वज़ह से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप देशद्रोही, पाकिस्तानी, हिंदू विरोधी कुछ भी घोषित किए जा सकते हैं। आपके ख़िलाफ़ कहीं भी मामला दर्ज़ किया जा सकता है, आपको गिरफ़्तार करके जेल भेजा जा सकता है। आपके ऊपर राजद्रोह और आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धाराएँ लगाकर आपको अनंतकाल तक जेल में रखा जा सकता है।
लड़ी होगी हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए लड़ाई, दी होगी आज़ादी के नाम पर शहादत, मगर आज इसकी बात करना भी गुनाह है। यह नाक़ाबिले बर्दाश्त है कि कोई आज़ादी का नारा लगाए। हमारा मीडिया उसका चरित्र हनन करने में एक क्षण की भी देर नहीं करेगा। वह देशवासियों को इतना भड़का देगा कि वे आपकी मॉब लिंचिंग कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम ख़तरों के बावजूद बात तो करनी ही होगी और खुलकर करनी होगी। अगर आज़ादी बचानी है तो सारे जोखिम उठाने होंगे।
जानी-मानी लेखिका अरुंधति रॉय लंबे समय से यही कर रही हैं। वह बार-बार सत्ता को चुनौती देते हुए आज़ादी की बात करती हैं। अपनी आज़ादी की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों, समुदायों की आज़ादी की जिन्हें किसी न किसी रूप में उससे वंचित किया जा रहा है। वे आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक भी हैं। वह इस क्रम में हर तरह के वर्चस्व और प्रभुत्व को चुनौती देती हैं। उनके निशाने पर वह हर तरह की सत्ता है, जो अत्याचार और शोषण पर टिकी है। कथा साहित्य से लेकर सम-सामयिक लेखों तक आज़ादी की यही माँग और जद्दोजहद उनके लेखन में फैली हुई है।
उनकी क़िताब आज़ादी दरअसल, 2018 से लेकर 2020 तक लिखे गए लेखों या दिए गए व्याख्यानों का संकलन है। अरुंधति अँग्रेज़ी की लेखिका हैं इसलिए ज़ाहिर है कि हिंदी में अनुवाद किया गया है। लेकिन रेयाज़ुल हक़ का अनुवाद बहुत ही सहज और तरल है, लिहाज़ा भाषा कहीं अवरोध बनकर खड़ी नहीं होती।
अरुंधति महसूस करती हैं कि ये दो साल दो सौ साल की तरह हैं और क़िताब को पढ़ने के बाद सचमुच में ऐसा लगता है कि हम एक पूरे वक़्त को पढ़ रहे हैं। कथेतर साहित्य होने के बावजूद संकलित लेख क़िस्से-कहानियों की तरह दिलचस्प और आँख खोलने वाले हैं। इसकी वज़ह यह है कि वे संवेदनाओं से भरे हुए हैं। उनमें तरह-तरह के वास्तविक किरदार हैं, ढेर सारे मगर बहुत ज़रूरी ब्यौरे विशिष्ट व्याख्याओं के साथ मौजूद हैं। कई बार वह अपने उपन्यासों को भी चर्चा में ले आती हैं।
दरअसल, अरुंधति की अपनी एक ख़ास लेखन शैली है, जिसमें वह तरह-तरह से संवाद करती नज़र आती हैं। कई जीवंत पात्रों और घटनाओं के ज़रिए वह सवाल करती हैं और उनके जवाब ढूँढ़ती हैं। जब वह तल्ख होती हैं तो तंज़ का सहारा भी लेती हैं।
वह जिस विषय को लेती हैं, उसकी परतें उघाड़ती जाती हैं और इस क्रम में कुछ ऐसा सामने आता है जिसकी तरफ़ हमने ध्यान ही नहीं दिया होता। यह एक संवेदनशील मनुष्य और रचनाकार की दृष्टि का कमाल होता है, जो बिरला ही देखने को मिलता है।
मसलन, क़िताब के पहले ही लेख को ले लीजिए। यह लेख 2018 में ब्रिटिश लायब्रेरी में दिया गया उनका व्याख्यान है। वह इसमें अपनी ज़ुबान का सवाल उठाती हैं और फिर भारत में भाषाओं की स्थिति पर से परदा उठाती जाती हैं। वह लिखती हैं, भारत में 780 ज़ुबानें हैं जिनमें से केवल बाईस को संविधान में स्वीकृति दी गई है जबकि अड़तीस ये दर्ज़ा पाने का इंतज़ार कर रही हैं। इनमें से हरेक का उपनिवेश बनाने या उपनिवेश बन जाने का अपना इतिहास है। ऐसी ज़ुबानें बहुत कम हैं जो सिर्फ़ पीड़ित या सिर्फ़ अपराधी हैं। इसी संदर्भ में वे हिंदी-उर्दू को लेकर चलने वाली सांप्रदायिक राजनीति को भी परखती हैं।
अरुंधति मानती हैं कि भारत में कुछ भी सुलझा हुआ नहीं है और न होगा। बीस साल बाद अपना दूसरा उपन्यास ‘द मिनिस्ट्री ऑफ़ अटमोस्ट हैपीनेस’ को पूरा करने के बाद भी वह भाषा को लेकर उलझन में थीं। उन्होंने महसूस किया कि एक उपन्यास का कोई दुश्मन हो सकता है तो एक राष्ट्र, एक धर्म और एक ज़ुबान का विचार। ज़ाहिर है कि वे हर स्तर पर बहुलता और विविधता को प्रतिष्ठित करना चाहती हैं। इससे उनके अंदर एक असमंजस भी पैदा होता है जो उपन्यास का आवरण पृष्ठ टाइप करते हुए प्रकट होता है। उनको ये खयाल आया कि एक भाषा की जगह वह लिखें कि मूल ज़ुबान से अरुंधति रॉय द्वारा अनूदित। ऐसा इसलिए कि ये उपन्यास कई भाषाओं में सोचा गया और ये अनुवाद ही था जिसकी बुनियाद पर उपन्यास लिखा गया।
वास्तव में वह ज़ुबान को भी अपनी आज़ादी के रूप में चिन्हित कर रही होती हैं। वह लिखती हैं-
“
द गॉड ऑफ़ स्माल थिंग्स’ लिखते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी रग़ों में ख़ून अधिक आज़ादी के साथ बहता है। ये एक बेपनाह राहत की बात थी कि मैंने आख़िर में एक ज़ुबान पा ली थी, जो मेरी अपनी ज़ुबान जैसी महसूस हुई।
अरुंधति रॉय
अरुंधति यहाँ आज़ादी की ज़ुबान की बात कर रही हैं। उस आज़ादी की ज़ुबान जो उनके तमाम लेखन में निर्बाध बहती देखी जा सकती है।
अरुंधति की आज़ाद ज़ुबान हर जगह आज़ादी तलाशती है। हमारे शिकस्ता ज़ख़्मी दिल लेख में वे पुलवामा हमले और उसके चुनावी दोहन के प्रसंग को उठाते हुए कश्मीरियों की माँग पर आ जाती हैं। हालाँकि आज के हिंदुस्तान में इस तरह का सवाल करना किसी देशद्रोह से कम नहीं है, मगर वह पूछती हैं कि जो भारतीय ब्रिटिश हुकूमत से अपनी आज़ादी की लड़ाई के गुण गाते हैं और एक तरह से उसकी रहनुमाई करने वालों की पूजा तक करते हैं वे अजीबोग़रीब त़रीक़े से कश्मीरियों को लेकर आँखें मूंद लेते हैं, जबकि कश्मीरी भी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं।
कश्मीर आज़ाद खयाल अरुंधति के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला मुद्दा है। एक अन्य लेख ख़ामोशी सबसे बुलंद आवाज़ में धारा 370 को हटाए जाने के पहले से अगले कई महीनों तक कश्मीर को क़ैद करने का वर्णन करती हैं।
वह दूरदर्शन पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करते हुए कहती हैं- जब वह जज़्बाती भाषण दे रहे थे तो उन्होंने यह नहीं बताया कि कश्मीरियों को घरों में बंद रहने की ज़रूरत क्यों है, और क्यों उन्हें सारी दुनिया से काट दिया गया है। उन्होंने वह नहीं बताया कि जिस फ़ैसले से उन लोगों को इतना फ़ायदा होने की बात कही जा रही है, वह उन लोगों के बिना सलाह लिए क्यों लिया गया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि भारतीय लोकतंत्र के महान तोहफ़े एक ऐसी अवाम के किस काम आएँगे जो फ़ौजी कब्ज़े में रह रही है।
‘द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स’ उपन्यास लिखने के बाद अरुंधति ने अपना पहला लेख लिखा था ‘द एंड ऑफ़ इमेजिनेशन’। ये वाजपेयी सरकार द्वारा परमाणु बम का परीक्षण करने पर लिखा गया था। उन्होंने इसमें कहा, “परमाणु होड़ में शामिल होकर हम अपनी कल्पना का उपनिवेशीकरण कर देंगे-अगर अपने दिमाग़ में परमाणु बम लगाने का विरोध करना हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है तो मैंने कहा, मैं मुल्क से अलग होती हूँ। मैं खुद को एक आज़ाद, खानाबदोश गणतंत्र घोषित करती हूँ।“
हिंदू राष्ट्रवाद की बेलगाम रफ़्तार को वह अंत की इत्तला मानती हैं। यह अंत आज़ादी का है, लोकतंत्र का है। ये केवल कश्मीर तक महदूद नहीं है, पूरा देश इसकी ज़द में है। कश्मीर से विशेष दर्ज़ा छीनने से लेकर सीएए, एनआरसी, मॉब लिंचिंग तक तमाम गतिविधियाँ इसी की सूचना दे रही हैं। इस सूचना को लोग ग्रहण नहीं कर रहे हों तो और बात है। ये तमाम फ़ैसले दरअसल, अल्पसंख्यकों को निहत्था करने के लिए हैं, उनसे राजनीतिक अधिकार छीनकर असहाय बनाने के लिए हैं। और बीजेपी ने यह कर दिखाया है। वह मुसलमानों के वोटों की परवाह किए बिना जीतकर दो बार सत्ता पर काबिज़ हो चुकी है।
वह असम में एनआरसी के नाम पर किए गए अत्याचारों का बहुत ही मार्मिक वर्णन करती हैं। बताती हैं कि कैसे लाखों हिंदू-मुसलमान अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कंगाल हो गए, बरबाद हो गए। इसके बावजूद बहुत से लोग अभी भी संदेह के घेरे में खड़े अनिश्चितता में जीवन गुज़ार रहे हैं।
यहीं वह हिंदू राष्ट्र में दलितों की स्थिति को भी बयान करते हुए हरियाणा के एक दलित युवा दयाचंद की कहानी सुनाती हैं। एक सवर्ण हिंदुओं की भीड़ ने जब पाँच दलित युवकों को पीट-पीटकर मार डाला तो वह अपमान और ग़ुस्से से भर उठा और उसने इसलाम कबूल कर लिया।
उन्होंने सद्दाम हुसैन से प्रेरित होकर उसने अपना नाम भी सद्दाम रख लिया। इसी तरह उन्होंने और भी दलितों के धर्मांतरण के ब्यौरे दिए हैं। ये ब्यौरे यही बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र किन हिंदू जातियों का स्वप्न है और उसमें बाक़ी जातियों की आज़ादी का क्या हश्र होगा।
वह दिल्ली दंगों की बात करते हुए कोरोना महामारी तक जाती हैं और हर जगह पाती हैं कि मौजूदा निज़ाम भेदभाव और हिंसा पर टिका है। वह ‘हम’ और ‘वे’ की अवधारणा पर काम कर रहा है। जो हिंदुत्व के साथ नहीं हैं वे देशद्रोही हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए और नहीं मानेंगे तो हम उन्हें झूठे आरोपों मे जेल में डाल देंगे (जैसे भीमा कोरेगाँव और दूसरे बहुत से मामलों में किया गया) या दंगों में मरवा देंगे। सत्ता का यह निर्मम रूप हमें नोटबंदी और फिर कोरोना काल में थोपे गए लॉकडाउन में भी देखने को मिलता है।
दुनिया अभी इसे उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। उसे लगता है कि हिंदुत्व बहुत आगे नहीं जाएगा या जा सकता। मगर हिंदू राष्ट्रवाद के पास आरएसएस जैसा विशाल संगठन है जो दुनिया में कहीं किसी भी विचारधारा के पास नहीं है और वह कुछ भी करने की हैसियत रखता है, ख़ास तौर पर तब जब सत्ता भी उसके पास हो और सत्ता के तंत्रों के इस्तेमाल की सहूलियत भी।
कुल मिलाकर ‘आज़ादी’ में संकलित लेखों में अरुंधति रॉय तानाशाही के दौर में आज़ादी को बचाने और उसके असली मायनों को समझने का आग्रह करती हैं।





















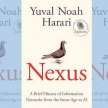

















अपनी राय बतायें