गांधी जब हमेशा के लिए भारत वापस आ गए और अपने छूटे हुए देश को उन्होंने ग़ौर से देखना शुरू किया तो उन्हें प्रायः निराशा का सामना करना पड़ा। यह जितना अंग्रेज़ी हुक़ूमत के ज़ुल्म के अफ़सोस का था, उससे ज़्यादा अपने देशवासियों की जड़ता का।
धर्म का गांधी-विचार
गांधी का अब तक का वयस्क जीवन भारत से बाहर इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में गुजरा था। कहा जा सकता है कि ईसाइयत और फिर इसलाम के संसर्ग में उन्होंने अपने हिंदूपन को पहचाना। ‘गीता’ का अध्ययन भी उन्होंने उनके आग्रह पर किया जो हिंदू न थे। बाइबिल और कुरआन का गहरा अध्ययन गाँधी ने किया और वे इन दोनों धर्मों के सन्देश के मुरीद भी हुए। लेकिन इसी चीज़ ने उनका विश्वास अपने धर्म के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी में दृढ़ किया। धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाने में क्या बहादुरी है? असल परीक्षा तो अपने धर्म में रहते हुए उससे लड़ते रहने में है।
धर्म को जैसा मिला वैसा ही ग्रहण करके आजीवन उसका पालन करते रहना भी कुछ नहीं, आपके चलते उस धर्म ने क्या बदला, यह असल बात है। गांधी जितना अंग्रेजों से लड़े, उससे कहीं ज़्यादा अपने धर्म से। यह भी कहा ही जाना चाहिए कि अंग्रेज शायद गांधी से अधिक सभ्यता से पेश आए, हिंदुओं ने गांधी को क्षमा नहीं किया। वे दोनों को ही कह रहे थे कि वे अपने बारे में अपने दावों पर विचार करें। क्या पश्चिमी सभ्यता सचमुच सभ्यता कहलाने योग्य है? उसी तरह क्या सनातन धर्म में कुछ भी आध्यात्मिक रह गया है?
धर्म का गांधी-विचार तुलनात्मक तो है लेकिन एक को दूसरे से बेहतर या हीन मानने से वे इनकार करते हैं। भारत लौटकर अपने धर्मावलंबियों से उनकी एक बड़ी निराशा इस कारण थी कि वे गीता का ‘ग’ भी नहीं जानते थे।
इसका अर्थ यह था कि अपने धर्म को आयत्त करने के लिए वे ज़रा भी श्रम नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्हें यह गुमान था कि उनका धर्म बाकी सबसे श्रेष्ठ है। अपने धर्म के प्रति आस्था अगर अन्य धर्मों से घृणा की तरफ ले जाए तो वास्तव में धर्म की नहीं अपनी प्रधानता साबित करने की ही कोशिश है। यह अहंकार है और आत्मग्रस्तता भी है।
हिंदुओं के लिए इसलाम ख़ास दिलचस्पी का धर्म रहा है। बल्कि कहा जा सकता है कि जितना वे अपने धर्म, उसे सनातन कहें या हिंदू, चर्चा नहीं करते, उतना और उससे कहीं ज्यादा वे इसलाम और मुसलमानों के बारे में चिंतित रहते हैं। पिछले दिनों हिमांशु कुमार से बात करते हुए उनके चेताने पर ध्यान आया कि बुतशिकनी कोई इसलाम की ही ख़ासियत या कुछ लोगों की निगाह में 'बुराई' हो, ऐसा नहीं। खुद हिंदू परम्पराओं में मूर्ति पूजा को मूर्खता यानी एक कुरीति माननेवाले पंथ रहे हैं।
नाम बड़ा कि रूप? नाम और रूप में चुनाव करना हो तो नाम को तरजीह देनेवाले और उसे किसी रूप में आबद्ध करके रूढ़ न करनेवालों की लंबी फ़ेहरिस्त उस सिलसिले से खोजी जा सकती है, जिसे हिंदू नाम से अभिहित किया जाता है। सबसे निकट ‘आर्य समाज’ के आन्दोलन को ही याद किया जा सकता है। क्या वह मूर्तिपूजकों से श्रेष्ठ साबित हुआ?
पाया गया कि आर्य समाज के प्रभाववाले क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के लिए सबसे अधिक उपजाऊ साबित हुए। संघ का मूलाधार जितना हिंदू धर्म में श्रद्धा नहीं है, उतना हिन्दुओं की अन्य मतावलंबियों पर प्राकृतिक श्रेष्ठता का दंभ है और यह विचार कि भारत नामक भौगोलिक विस्तार पर उनका दैवी अधिकार है।
एक धारणा यह है कि मूर्तिपूजक अधिक उदार और समावेशी होते हैं क्योंकि वे विविध प्रकार के रूपों की आराधना समान भाव से कर सकते हैं और उनमें इस कारण कट्टरता कम होनी चाहिए। लेकिन मूर्तिपूजकों के इतिहास ने इसे ग़लत साबित किया है।
प्रेमचंद आर्य समाज से प्रभावित थे। उस समय माना गया था कि यह हिंदू धर्म को उसकी रूढ़ियों से मुक्त करने का अभियान है। लेकिन जो दिशा आर्य समाज ने अपनाई, उसने प्रेमचंद को उससे विरत कर दिया।
उनकी रुचि लेकिन धर्मों में बनी रही बावजूद इसके कि ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास न था। धर्म से वे उदासीन नहीं रह सकते थे, क्योंकि यह प्रथमतः और अंतिम रूप से मानवीय और सामाजिक व्यापार था।
भारत में धर्म के प्रश्न से टकराए बिना किसी भी तरफ बढ़ना मुमकिन न था। ख़ासकर भारत में इसलाम के सवाल से जूझना तो हरेक के लिए लाजिमी था। इस विषय पर विचार करने का तरीका क्या हो? ‘हिन्दू-मुसलिम एकता’ नामक निबंध में प्रेमचंद इस विषय पर बात करने की मुश्किल बताते हैं,
'दिलों में गुबार भरा हुआ है, फिर मेल कैसे हो? मैली चीज़ पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, यहाँ तक कि जब तक दीवाल साफ़ न हो, उसपर सीमेंट का पलस्तर भी नहीं ठहरता। हम ग़लत इतिहास पढ़-पढ़कर एक दूसरे के प्रति तरह-तरह की ग़लतफहमियाँ दिल में भरे हुए हैं, और उन्हें किसी तरह दिल से नहीं निकालना चाहते, मानो उन्हीं पर हमारे जीवन का आधार हो।'
इतिहास से प्रेमचंद की विरक्ति प्रसिद्ध है। कारण उनके लिए बहुत साफ़ था।इतिहास में जाकर अपने वर्तमान द्वेष को पुष्ट करने के लिए दोनों ही उदाहरण खोजकर ला सकते हैं और किसने किसको जलील किया, इस झगड़े का निबटारा कभी न होगा,
'प्राचीन हमारे भविष्य का पथ प्रदर्शक हुआ करता है। प्राचीन को दूषित करके, उसमें द्वेष और भेद का कीना भरकर भविष्य को भुलाया सकता है। वही भारत में हो रहा है।' हाल में अमर्त्य सेन ने दिल्ली में एक संवाद में जो कहा, उसे प्रेमचंद अरसा पहले कह चुके थे,
'यह बात हमारे अंदर ठूँस दी गई है कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से दो विरोधी दलों में विभाजित रहे हैं, हालाँकि ऐसा कहना सत्य का गला घोंटना है।'
इसलाम के प्रति आकर्षण
प्रेमचंद जोर देकर कहते हैं,
'यह बिलकुल ग़लत है कि इसलाम तलवार के बल से फैला। तलवार के बल से कोई धर्म नहीं फैलता, और कुछ दिनों के लिए फैल भी जाए, तो चिरजीवी नहीं हो सकता।'
भारत में इसलाम के प्रति जनता के आकर्षण का कारण इसमें उसूली तौर पर ऊँच-नीच की भावना का विरोध और समानता की सर्वोच्चता थी। प्रेमचंद की व्याख्या इसलाम के भारत में प्रसार की बहुतों से अलग नहीं, लेकिन उसकी भावना को समझने की ज़रूरत है। भारत में ऊँच-नीच के प्रचलित सिद्धांत को बौद्ध धर्म ने चुनौती दी। इसके कारण जिन्हें नीचा माना जाता था उन्होंने आत्म सम्मान पा लिया। बौद्ध धर्म के कमजोर पड़ने के साथ,
'नीची जातियों पर फिर वहीं पुराना अत्याचार शुरू हुआ, बल्कि और ज़ोरों के साथ। ऊँचों ने नीचों से उनके विद्रोह का बदला लेने की ठानी।'
जिन्होंने एक बार बराबरी का मज़ा चख लिया था, वे इस अत्याचार को चुपचाप नियम मान लें, यह संभव न था।
'यह खींच-तान चल ही रही थी कि इसलाम ने नए सिद्धांतों के साथ पदार्पण किया। वहाँ...छोटे-बड़े, ऊँच-नीच की कैद न थी। इसलाम की दीक्षा लेते ही मनुष्य की सारी अशुद्धियाँ, सारी अयोग्यताएँ मानो धुल जाती थीं। वह मसजिद में इमाम के पीछे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता था।' इसलिए इसलाम का हर्ष के साथ स्वागत हुआ।
'तो इसलाम तलवार के बल से नहीं, बल्कि अपने धर्म-तत्त्वों की व्यापकता के बल से फैला। इसलिए फैला कि उसके यहाँ मनुष्य मात्र के अधिकार समान हैं।' प्रेमचंद इसी कारण भारत के इतिहास को इसलाम और हिंदू धर्म के द्वंद्व के वृत्तान्त के रूप में पढ़ने के खिलाफ हैं। वे इतिहासकार प्रोफ़ेसर मोहम्मद हबीब को अपने मत के पक्ष में उद्धृत करते हैं,
'...उस ज़माने का हिंदू मजहब संगठित और शक्तिशाली था। उसके साथ मुसलमान बादशाह इसलिए रवादारी बरतते थे कि इसके सिवा दूसरी राह न थी।..उनके लिए साम्प्रदायिक संघर्ष का फल तबाही के सिवा कुछ न होता। यह विचित्र बात है कि मध्यकालीन इतिहास के राजनैतिक या ऐतिहासिक साहित्य में हिंदू-मुसलिम द्वंद्व का कोई छोटे से छोटा प्रमाण नहीं मिलता।...असली हिंदू-मुसलिम लडाई तो वास्तव में कभी हुई ही नहीं।'
हम अभी इस प्रश्न पर सिर्फ प्रेमचंद की विचार-पद्धति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ‘साम्प्रदायिक मताधिकार की घोषणा’ शीर्षक लेख से आज कई लोग अचंभित हो जा सकते हैं। मताधिकार के प्रसंग में मुसलमानों को अतिरिक्त वेटेज देने पर हिंदुओं और सिखों में असंतोष पैदा हुआ। प्रेमचंद की निगाह इतनी साफ़ क्यों है?
'...यह क्यों समझ लिया जाय कि मुसलमानों में बहुमत से हिंदू या सिक्खों के हितों की हानि होगी। मुसलमानों का भारत पर कई सदियों तक राज रहा है। अगर मुसलमान उस ज़माने में हिन्दुओं को न कुचल सके तो अब इसकी कोई संभावना नहीं रही।' प्रेमचंद और भी आगे बढ़कर हिंदुओं और सिक्खों को उत्साहित करते हैं कि वे विशेषाधिकार मिलने पर मुसलमानों को बधाई दें न कि उनसे मुँह फेर लें।
'जब मुसलमानों को कुछ अधिकार अधिक मिल जाते हैं तो हमें क्यों तुरंत यह विचार होता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। कारण यही है कि हम मुँह से चाहे राष्ट्रीयता की दुहाई दें, दिल में हम सभी सम्प्रदायवादी हैं और हरेक बात को संप्रदाय की निगाह से देखते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि जब कोई साम्प्रदायिक दंगा हो जाता है, तो हम तुरंत यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि उस दंगे में कितने हिंदू हताहत हुए और कितने मुसलमान। अगर हिन्दुओं की संख्या अधिक होती है, तो हम कितने उत्तेजित हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर मुसलमानों की संख्या अधिक होती, तो हम आराम की साँस लेते हैं। यह मनोवृत्ति राष्ट्रीयता का गला घोंटनेवाली है। हमें इस मनोवृत्ति का मूलोच्छेद करना होगा अन्यथा हमारा राष्ट्र मधुर स्वप्न ही रहेगा।'
धर्म का उज्ज्वल पक्ष
यह मनोवृत्ति कैसे खत्म हो? प्रश्न जितना राजनीतिक है उससे अधिक अन्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण का है। प्रेमचंद ने सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानों को पात्र बनाकर कहानियाँ और उपन्यास नहीं लिखे।
प्रेमचंद के लिए खुद हिंदू धर्म और इसलाम अपने आप में पात्र या चरित्र थे। इसलाम को लेकर लिखी उनकी कहानियों को पढ़ें तो नज़रिया उत्सुकता का तो है उस धर्म के प्रति, उसके साथ हमेशा ही धर्म के रूप में उसके उज्ज्वल पक्ष के उद्घाटन पर ध्यान है।
‘मंदिर और मसजिद’ के इतरत अली में गहरी धार्मिक नैतिकता है। 'दिल की रानी’ का हबीब भी उस नैतिकता के कारण ईसाइयों को उनके धार्मिक विश्वासों के पालन का अधिकार देता है और तैमूर उसका साथ देता है। ‘नबी का न्याय’ में भी न्याय के सिद्धांत में पक्षपात से नबी के इनकार पर ही ज़ोर है।
प्रेमचंद क्यों इसलाम के इस पक्ष की ओर ही ध्यान दिलाते हैं? ‘क्षमा’ इसलाम को पात्र बनाकर लिखी गई उनकी एक और कहानी है। कहानी की शुरुआत में ही इसलाम और ईसाइयत के बीच के संघर्ष की पृष्ठभूमि को सामने रख दिया जाता है:
'मुसलमानों को स्पेन-देश पर राज्य करते कई शताब्दियाँ बीत चुकी थीं। कलीसाओं की जगह मसजिदें बनती जाती थीं, घंटों की जगह अजान की आवाजें सुनाई देती थीं। ग़रनाता और अलहमरा में वे समय की नश्वर गति पर हँसनेवाले प्रासाद बन चुके थे, जिनके खंडहर अब तक देखनेवालों को अपने पूर्व ऐश्वर्य की झलक दिखाते हैं।' धर्म सांसारिक अहंकार का शिकार कितनी आसानी से हो जाता है! वह तो अनश्वर है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नश्वरचिह्नों के बिना जैसे घोषित ही नहीं हो सकती।
इसलाम विजेता है और अभिजन ईसाई उसकी शरण में जा रहे हैं, लेकिन एक अभी भी है जिसने इस फ़तहयाब इसलाम के आगे सर नहीं झुकाया है। जो बलशाली है उसके बल के कारण उसकी शरण में जाना बुद्धिमानी हो सकती है, वीरता नहीं। और वीरता प्रेमचंद के लिए उतना ही बड़ा मूल्य है, जितना बराबरी और न्याय।
'जो ईसाई-नेता अब तक मुसलमानों के सामने सिर न झुकाते थे, और अपने देश में स्वराज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे उनमें एक सौदागर दाऊद भी था। दाऊद विद्वान और साहसी था। वह अपने इलाके में इसलाम को कदम न जमाने देता था। दीन और निर्धन ईसाई विद्रोही देश के अन्य प्रांतों से आकर उसके शरणागत होते थे और वह बड़ी उदारता से उनका पालन-पोषण करता था।'
विद्रोह हमेशा ही आदर के योग्य है। बहस इसलाम और ईसाइयत के बीच गुणों की श्रेष्ठता की नहीं है। दाऊद ताक़त के आगे सर नहीं झुकाता और धर्म का कर्तव्य जो उदारता की बुनियाद पर टिका है, नहीं भूलता। उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। वह धर्म कर्तव्य है, जो किया ही जाना चाहिए अगर आप इंसान हैं।
'मुसलमान दाऊद से सशंक रहते थे। वे धर्म-बल से उस पर विजय न पाकर उसे अस्त्र-बल से परास्त करना चाहते थे; पर दाऊद कभी उनका सामना न करता। हाँ, जहाँ कहीं ईसाइयों के मुसलमान होने की खबर पाता, हवा की तरह पहुँच जाता और तर्क या विनय से उन्हें अपने धर्म पर अचल रहने की प्रेरणा देता।' अस्त्र बल की जगह तर्क और विनय और अपने विचारों में दृढ़ता!
दाऊद आखिरकार गरनाता में पनाह लेता है जो ‘इसलामी राजधानी’ है। अपने गुणों के कारण ही लाख खोजने पर भी कोई मुसलमानों को उसका सुराग नहीं देता। आखिर एक दिन वह पकड़ा जाता है।
'एक दिन एकांतवास से उकताकर दाऊद ग़रनाता के एक बाग में सैर करने चला गया। संध्या हो गयी थी। मुसलमान नीची अबाएँ पहने, बड़े-बड़े अमामे सिर पर बाँधे, कमर से तलवार लटकाये रबिशों में टहल रहे थे। स्त्रियाँ सफेद बुरके ओढ़े, जरी की जूतियाँ पहने बेंचों और कुरसियों पर बैठी हुई थीं। दाऊद सबसे अलग हरी-हरी घास पर लेटा हुआ सोच रहा था कि वह दिन कब आयेगा जब हमारी जन्मभूमि इन अत्याचारियों के पंजे से छूटेगी! वह अतीत काल की कल्पना कर रहा था, जब ईसाई स्त्री और पुरुष इन रबिशों में टहलते होंगे, जब यह स्थान ईसाइयों के परस्पर वाग्विलास से गुलजार होगा।' तर्क-वितर्क
ईसाइयत बेहतर या इसलाम? फिर बहस इसकी नहीं। क्या इसलाम के बेहतर मूल्यों के कारण मुसलमानों को अधिकार मिल जाता है कि वे ईसाईयों पर कब्जा कर लें और वे धर्म बदल लें? आगे का संवाद सुनें। तर्क-वितर्क में वाग्विदग्धता के नमूनों के कारण भी।'सहसा एक मुसलमान युवक आकर दाऊद के पास बैठ गया। वह उसे सिर से पाँव तक अपमानसूचक दृष्टि से देखकर बोला - क्या अभी तक तुम्हारा हृदय इसलाम की ज्योति से प्रकाशित नहीं हुआ?
दाऊद ने गम्भीर भाव से कहा - इसलाम की ज्योति पर्वत-शृंगों को प्रकाशित कर सकती है। अँधेरी घाटियों में उसका प्रवेश नहीं हो सकता।
उस मुसलमान अरब का नाम जमाल था। यह आक्षेप सुनकर तीखे स्वर में बोला - इससे तुम्हारा क्या मतलब है ?
दाऊद - इससे मेरा मतलब यही है कि ईसाइयों में जो लोग उच्च-श्रेणी के हैं, वे जागीरों और राज्याधिकारों के लोभ तथा राजदंड के भय से इसलाम की शरण में आ सकते हैं; पर दुर्बल और दीन ईसाइयों के लिए इसलाम में वह आसमान की बादशाहत कहाँ है जो हज़रत मसीह के दामन में उन्हें नसीब होगी! इसलाम का प्रचार तलवार के बल से हुआ है, सेवा के बल से नहीं।'
'जमाल अपने धर्म का अपमान सुनकर तिलमिला उठा। गरम होकर बोला - यह सर्वथा मिथ्या है। इसलाम की शक्ति उसका आंतरिक भ्रातृत्व और साम्य है, तलवार नहीं।
दाऊद - इसलाम ने धर्म के नाम पर जितना रक्त बहाया है, उसमें उसकी सारी मसजिदें डूब जायँगी।
जमाल - तलवार ने सदा सत्य की रक्षा की है।
दाऊद ने अविचलित भाव से कहा - जिसको तलवार का आश्रय लेना पड़े, वह सत्य ही नहीं।
जमाल जातीय गर्व से उन्मत्त होकर बोला - जब तक मिथ्या के भक्त रहेंगे, तब तक तलवार की जरूरत भी रहेगी।
दाऊद - तलवार का मुँह ताकनेवाला सत्य ही मिथ्या है।'
यह बहस प्रेमचंद की इस प्रकार की कहानियों में लगातार चलनेवाली है : तलवार का मुँह ताकनेवाला सत्य मिथ्या है! बहस आखिरकार भाषा से निकलकर अस्त्रों की शरण में चली जाती है।
'दोनों ने तलवारें खींच लीं। एक-दूसरे पर टूट पड़े। अरब की भारी तलवार ईसाई की हलकी कटार के सामने शिथिल हो गयी। एक सर्प की भाँति फन से चोट करती थी, दूसरी नागिन की भाँति उठती थी। लहरों की भाँति लपकती थी, दूसरी जल की मछलियों की भाँति चमकती थी। दोनों योद्धाओं में कुछ देर तक चोटें होती रहीं। सहसा एक बार नागिन उछलकर अरब के अंतस्तल में जा पहुँची। वह भूमि पर गिर पड़ा।'
प्रेमचंद की सुख़नसाजी
आप से फिर गुजारिश है, प्रेमचंद की सुख़नसाजी को नज़रअंदाज न करें। कहानी में भाषा के अलावा न तो भाव कहीं और है न अर्थ न आशय!
जो अरब मारा गया, उसका नाम जमाल था। उसके गिरते ही आस पास इकट्ठा मुसलमान दाऊद को घेर लेते हैं:
'उधर अरबों की रक्त-पिपासा प्रतिक्षण तीव्र होती जाती थी। यह केवल एक अपराधी को दंड देने की चेष्टा न थी। जातीय अपमान का बदला था। एक विजित ईसाई की यह हिम्मत कि अरब पर हाथ उठाये! ऐसा अनर्थ!' रक्त-पिपासा, जातीय अपमान का प्रतिशोध! कोई विजित किसी विजेता पर हाथ कैसे उठा सकता है?दाऊद घिर गया है। फिर प्रेमचंद की मुहावरेदार भाषा:
'जिस तरह पीछा करनेवाले कुत्तों के सामने गिलहरी इधर-उधर दौड़ती है, किसी वृक्ष पर चढ़ने की बार-बार चेष्टाकरती है, पर हाथ-पाँव फूल जाने के कारण बार-बार गिर पड़ती है, वही दशा दाऊद की थी। दौड़ते-दौड़ते उसका दम फूल गया; पैर मन-मन भर के हो गये। कई बार जी में आया इन सब पर टूट पड़े और जितने महँगे प्राण बिक सकें, उतने महँगे बेचे; पर शत्रुओं की संख्या देखकर हतोत्साह हो जाता था।'
और यह वर्णन भी प्रेमचंद की कलम ही कर सकती थी:
'दाऊद को अब इस संग्राम में खिलाड़ियों का-सा आनंद आने लगा। यह निश्चित था कि उसके प्राण नहीं बच सकते, मुसलमान दया करना नहीं जानते, इसलिए उसे अपने दाँव-पेंच में मजा आ रहा था। किसी वार से बचकर उसे अब इसकी खुशी न होती थी कि उसके प्राण बच गये, बल्कि इसका आनंद होता था कि उसने कातिल को कैसा ज़िच किया।' आखिरकार वह एक नीची दीवार फाँदकर भाग निकलता है! फौरी मौत से तो वह बच निकला है, लेकिन ख़तरा और उसके चारों ओर है।
'...चारों तरफ हलचल मची हुई है, शत्रुओं का दल मशालें लिये झाड़ियों में घूम रहा है; नाकों पर भी पहरा है, कहीं निकल भागने का रास्ता नहीं है। दाऊद एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्योंकर जान बचे। उसे अपनी जान की वैसी परवा न थी। वह जीवन के सुख-दुख सब भोग चुका था। अगर उसे जीवन की लालसा थी, तो केवल यही देखने के लिए कि इस संग्राम का अंत क्या होगा? मेरे देशवासी हतोत्साह हो जायेंगे, या अदम्य धैर्य के साथ संग्रामक्षेत्र में अटल रहेंगे।' दाऊद अब किसी आबादी तक पहुँच जाना चाहता है। वह इसलिए कि
'...निर्जनता किसी की आड़ नहीं कर सकती। बस्ती का जनबाहुल्य स्वयं आड़ है।'
वह छिपते हुए निकलना चाहता है, लेकिन ताड़ लिया जाता है। वह फिर भागता है,
'बहुत दूर पर एक धुँधला-सा दीपक टिमटिमा रहा था। किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाऊँ। वह उस दीपक की ओर इतनी तेजी से दौड़ रहा था, मानो वहाँ पहुँचते ही अभय पा जायगा। आशा उसे उड़ाये लिये जाती थी। अरबों का समूह पीछे छूट गया; मशालों की ज्योति निष्प्रभ हो गयी। केवल तारागण उसके साथ दौड़े चले आते थे। अंत को वह आशामय दीपक के सामने आ पहुँचा।'
वह जहाँ पहुँचता है, वहाँ धर्म आधिपत्य के अहंकार से नहीं जल रहा, जिज्ञासा और श्रद्धा से प्रकाशित है,
'एक छोटा-सा फूस का मकान था। एक बूढ़ा अरब ज़मीन पर बैठा हुआ रेहल पर कुरान रखे उसी दीपक के मंद प्रकाश से पढ़ रहा था।'
फूस का मकान, बूढ़ा अरब, दीपक का मंद प्राकश और रेहल पर रखी कुरान!
'दाऊद आगे न जा सका। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वह वहीं शिथिल होकर गिर पड़ा। रास्ते की थकान घर पहुँचने पर मालूम होती है।
अरब ने उठकर कहा - तू कौन है ?
दाऊद - एक गरीब ईसाई। मुसीबत में फँस गया हूँ। अब आप ही शरण दें, तो मेरे प्राण बच सकते हैं।
अरब - खुदा-पाक तेरी मदद करेगा। तुम पर क्या मुसीबत पड़ी हुई है?
दाऊद - डरता हूँ कहीं कह दूँ तो आप भी मेरे खून के प्यासे न हो जायँ।
अरब - अब तू मेरी शरण में आ गया, तो तुझे मुझसे कोई शंका न होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, जिसे एक बार अपनी शरण में ले लेते हैं उसकी जिंदगी-भर रक्षा करते हैं।'
यह बूढ़ा भी इतरत अली का दूसरा अवतार है। कौन पहले और कौन बाद में?
'दाऊद - मैंने एक मुसलमान युवक की हत्या कर डाली है।
वृद्ध अरब का मुख क्रोध से विकृत हो गया, बोला - उसका नाम ?
दाऊद - उसका नाम जमाल था।
अरब सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसकी आँखें सुर्ख हो गयीं; गरदन की नसें तन गयीं; मुख पर अलौकिक तेजस्विता की आभा दिखायी दी, नथुने फड़कने लगे। ऐसा मालूम होता था कि उसके मन में भीषण द्वंद्व हो रहा है और वह समस्त विचार-शक्ति से अपने मनोभावों को दबा रहा है। दो-तीन मिनट तक वह इसी उग्र अवस्था में बैठा धरती की ओर ताकता रहा। अंत में अवरुद्ध कंठ से बोला -
'नहीं-नहीं, शरणागत की रक्षा करनी ही पड़ेगी। आह ! जालिम ! तू जानता है, मैं कौन हूँ। मैं उसी युवक का अभागा पिता हूँ, जिसकी आज तूने इतनी निर्दयता से हत्या की है। तू जानता है, तूने मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया है? तूने मेरे खानदान का निशान मिटा दिया है! मेरा चिराग गुल कर दिया!'
बूढ़ा बाप बेटे के मारे जाने पर भी अपने रसूल की हिदायत को नहीं भूल सकता। खून के बदले ख़ून का क़ानून है, लेकिन उसके ऊपर उसी रसूल पाक का आदेश कि शरणार्थी की रक्षा ही धर्म है:
'आह, जमाल मेरा इकलौता बेटा था। मेरी सारी अभिलाषाएँ उसी पर निर्भर थीं। वह मेरी आँखों का उजाला, मुझ अंधे का सहारा, मेरे जीवन का आधार, मेरे जर्जर शरीर का प्राण था। अभी-अभी उसे कब्र की गोद में लिटा आया हूँ। आह, मेरा शेर, आज खाक के नीचे सो रहा है।
'...मेरा जी चाहता है कि अपने दोनों हाथों से तेरी गरदन पकड़कर इस तरह दबाऊँ कि तेरी जबान बाहर निकल आये, तेरी आँखें कौड़ियों की तरह बाहर निकल पड़ें। पर नहीं, तूने मेरी शरण ली है, कर्तव्य मेरे हाथों को बाँधे हुए है, क्योंकि हमारे रसूल-पाक ने हिदायत की है, कि जो अपनी पनाह में आये, उस पर हाथ न उठाओ। मैं नहीं चाहता कि नबी के हुक्म को तोड़कर दुनिया के साथ अपनी आक़बत भी बिगाड़ लूँ। दुनिया तूने बिगाड़ी, दीन अपने हाथों बिगाड़ूँ? नहीं। सब्र करना मुश्किल है; पर सब्र करूँगा ताकि नबी के सामने आँखें नीची न करनी पड़ें।'
जमाल के पिता शेख हसन के लिए यह आसान न था:
'फिर चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ने लगा, लेकिन उसका मन पढ़ने में न लगता था। शत्रु से बदला लेने की प्रवृत्ति अरबों की प्रवृत्ति में बद्धमूल होती थी। खून का बदला खून था। ... उस प्रवृत्ति पर विजय पाना शेख हसन को असाध्य-सा प्रतीत हो रहा था। बार-बार प्यारे पुत्र की सूरत उसकी आँखों के आगे फिरने लगती थी, बार-बार उसके मन में प्रबल उत्तेजना होती थी कि चलकर दाऊद के खून से अपने क्रोध की आग बुझाऊँ।'
तो क्या प्रतिशोध की भावना अधिक प्रबल सिद्ध होगी? लेकिन क्या बदले की भावना अरबों, मुसलमानों की ही खासियत है?
'...अन्त को शेख हसन अधीर हो उठा। उसको भय हुआ कि अब मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता। उसने तलवार म्यान से निकाल ली और दबे पाँव उस कोठरी के द्वार पर आकर खड़ा हो गया, जिसमें दाऊद छिपा हुआ था। तलवार को दामन में छिपाकर उसने धीरे से द्वार खोला। दाऊद टहल रहा था। बूढ़े अरब का रौद्र रूप देखकर दाऊद उसके मनोवेग को ताड़ गया। उसे बूढ़े से सहानुभूति हो गयी। उसने सोचा, यह धर्म का दोष नहीं, जाति का दोष नहीं। मेरे पुत्र की किसी ने हत्या की होती, तो कदाचित् मैं भी उसके खून का प्यासा हो जाता। यही मानव प्रकृति है।'
आत्मस्वीकृति
आगे क़ातिल और मकतूल के पिता का संवाद है, लेकिन यह अमर संवाद है। हर धर्म को माननेवाले को इसे पढ़ना और गुनना होगा। यह वह आत्मस्वीकृति है जो शायद हर धर्म को एक न एक बार करना होगी:'अरब ने कहा - दाऊद, तुम्हें मालूम है बेटे की मौत का कितना गम होता है।
दाऊद - इसका अनुभव तो नहीं, पर अनुमान कर सकता हूँ। अगर मेरी जान से आपके उस गम का एक हिस्सा भी मिट सके, तो लीजिए, यह सिर हाजिर है। मैं इसे शौक से आपकी नज़र करता हूँ। आपने दाऊद का नाम सुना होगा।
अरब - क्या पीटर का बेटा ?
दाऊद - जी हाँ। मैं वही बदनसीब दाऊद हूँ। मैं केवल आपके बेटे का घातक ही नहीं, इसलाम का दुश्मन हूँ। मेरी जान लेकर आप जमाल के खून का बदला ही न लेंगे, बल्कि अपनी जाति और धर्म की सच्ची सेवा भी करेंगे।
शेख हसन ने गम्भीर भाव से कहा -
'दाऊद, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं जानता हूँ, मुसलमानों के हाथ ईसाइयों को बहुत तकलीफें पहुँची है, मुसलमानों ने उन पर बड़े-बड़े अत्याचार किये हैं, उनकी स्वाधीनता हर ली है! लेकिन यह इसलाम का नहीं, मुसलमानों का कसूर है। विजय-गर्व ने मुसलमानों की मति हर ली है। हमारे पाक नबी ने यह शिक्षा नहीं दी थी, जिस पर आज हम चल रहे हैं। वह स्वयं क्षमा और दया का सर्वोच्च आदर्श है। मैं इसलाम के नाम को बट्टा न लगाऊँगा। मेरी ऊँटनी ले लो और रातो रात जहाँ तक भागा जाय, भागो। कहीं एक क्षण के लिए भी न ठहरना। अरबों को तुम्हारी बू भी मिल गयी, तो तुम्हारी जान की खैरियत नहीं। जाओ, तुम्हें खुदा-ए-पाक घर पहुँचावे। बूढ़े शेख हसन और उसके बेटे जमाल के लिए खुदा से दुआ किया करना।'
अपने बेटे को जिसके हाथों गँवा दिया उसे माफ़ करने का सुख कुछ और है। तलवार दाऊद के तन को सर कर सकती थी, बूढ़े शेख हसन के रहम ने दाऊद का दिल जीत लिया:
'दाऊद खैरियत से घर पहुँच गया; किंतु अब वह दाऊद न था, जो इसलाम को जड़ से खोदकर फेंक देना चाहता था। उसके विचारों में गहरा परिवर्तन हो गया था। अब वह मुसलमानों का आदर करता और इसलाम का नाम इज्जत से लेता था।'
ध्यान रहे अभी भी दाऊद ईसाई ही है,मुसलमान नहीं हुआ है।












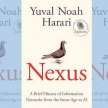













अपनी राय बतायें