'राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोढ़ है, उसी तरह जैसे मध्य-कालीन युग का कोढ़ साम्प्रदायिकता थी। नतीजा दोनों का एक है।' प्रेमचंद जिसे राष्ट्रीयता कहते हैं वह रवींद्रनाथ टैगोर के यहाँ राष्ट्रवाद है। टैगोर राष्ट्रवाद को आधुनिक समय और समाज की बीमारी मानते हैं। वह समुदायों के संकीर्ण स्वार्थों का संगठन है। यूरोप के इस आविष्कार को वे मनुष्य समाज के लिए अशुभ मानते हैं।
प्रेमचंद ने यह लेख 1933 में लिखा था। उसके 4 साल पहले भगत सिंह, नेहरू और सुभाष बाबू की तुलना करते हुए एक लेख लिख चुके थे। उन्हें सुभाष बाबू के विचारों में संकीर्ण राष्ट्रवाद की गंध मिली। नेहरू का खुला, उदार अंतरराष्ट्रीयतावाद उन्हें अपनी तरफ खींचता था।
राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता
भारत बाकी सारे देशों और राष्ट्रों से ख़ास और ऊपर है, दुनिया के लिए उसके पास कोई विशेष सन्देश है, यह सुभाष बाबू मानते हैं, लेकिन जैसे नेहरू को यह ख्याल नापसंद है वैसे ही भगत सिंह को भी। बनारसीदास चतुर्वेदी को 1930 के ख़त में वे लिख चुके हैं,
' मेरी आकांक्षाएँ कुछ नहीं हैं। इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज्य-संग्राम में विजयी हों।' जिसके लिए स्वराज्य सबसे बड़ा मक़सद है, वह राष्ट्रवाद को क्यों रोग मानता है?(आप कोढ़ शब्द के लिए प्रेमचंद और उनके वक्त को माफ़ कर दें) प्रेमचंद बड़ा सीधा सा कारण बताते हैं,
'साम्प्रदायिकता अपने घेरे के अन्दर पूर्ण शान्ति और सुख का राज्य स्थापित कर देना चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर जो संसार था, उसको नोचने-खसोटने में उसे ज़रा मानसिक क्लेश न होता था। राष्ट्रीयता भी अपने परिमित क्षेत्र के अन्दर राम-राज्य का आयोजन करती है।' आख़िरी वाक्य पर ध्यान दीजिए। अपने तंग दायरे में रामराज्य ही क्यों न स्थापित कर लिया जाए, प्रेमचंद को वह प्रेय नहीं। राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद अस्वीकार्य है क्योंकि वह संसार को राष्ट्रों या गिरोहों में बाँट देता है और सभी एक दूसरे को हिंसात्मक संदेह को दृष्टि से देखते हैं। संसार में शान्ति असंभव है जबतक यह परस्पर संदेह बना रहे।
नेहरू अंतररष्ट्रीयता के पैरोकार हैं, लेकिन उन्हें या रवींद्रनाथ टैगोर-जैसे व्यक्ति को संसार ड्रीमर या शेखचिल्ली मानकर उनका मज़ाक उड़ाता है। राष्ट्रवाद का रोग प्रेमचंद के अनुसार आधुनिक शिक्षा की देन है,
'जैसे शिक्षा से और कितनी ही अस्वाभाविकताएँ हमने अन्दर भर ली हैं, उसी तरह इस रोग को भी पाल लिया है।'
इससे मुक्ति के बिना मानवता का विकास संभव नहीं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बिना राष्ट्रवाद का स्तर पार किए अंतरराष्ट्रीयता तक पहुँचना संभव नहीं। प्रेमचंद इसे हास्यास्पद बताते हुए कहते हैं कि
'...जैसा श्रीकृष्ण मूर्ति ने अपने एक भाषण में कहा है, यह तो ऐसा ही है कि जैसे कोई कहे कि आरोग्यता स्थापित करने के लिए बीमार होना आवश्यक है।'
आवश्यकता हर किसी को मालूम होती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीयता स्थापित कैसे हो, इस सवाल का जवाब माकूल मिलता नहीं। क्या इसका आधार आध्यात्मिक होगा?
‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या ‘वेदान्त का एकात्मवाद’ या फिर इसलाम के भाईचारे के उसूल पहले से मौजूद हैं, लेकिन राष्ट्रों की दीवारें तो खड़ी हो ही गईं, यहाँ तक कि इसलाम का पालन करने वालों ने भी अलग-अलग राष्ट्रों के घेरे में खुद को क़ैद कर लिया।
धर्म इस विभेद को दूर न कर सका,
' उसने मनुष्य की स्वेच्छा पर विश्वास किया। लेकिन फल इसके सिवा कुछ न हुआ कि धर्मोपजीवियों की एक बहुत बड़ी संख्या पृथ्वी का भार हो गयी। समाज जहाँ था, वहीं खड़ा रह गया, नहीं, और पीछे हट गया। संसार में अनेक मतों और धर्मों और करोड़ों धर्मोपदेशकों के रहते हुए जितना वैमनस्य और ईर्ष्या भाव है उतना शायद पहले कभी न था।' प्रेमचंद इन उदात्त आध्यात्मिक आदर्शों की असफलता के कारण पर विचार करते हुए इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये रास्ते इस बात की उपेक्षा करते हैं कि
'यह जो प्राणी-प्राणी में भेद है, फूट है, वैमनस्य है, यह जो राष्ट्रों में परस्पर तनातनी हो रही है, इसका कारण अर्थ के सिवा और क्या है। अर्थ के प्रश्न को हल कर देना ही, राष्ट्रीयता के किले को ध्वंस कर सकता है।' अगर किसी की ग़ुलामी से खुद को आज़ाद करना है तो इस बात को नज़रअंदाज करके वह नहीं किया जा सकता। ‘क़ातिल’ नामक कहानी में माँ और बेटे के बीच की बहस में यह चर्चा इस तरह की जाती है,
'बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम समझते हो, अंग्रेजों को कत्ल कर देने से हम आज़ाद हो जायेंगे? हम अंग्रेजों के दुश्मन नहीं। हम इस राज्य प्रणाली के दुश्मन हैं। अगर यह राज्य-प्रणाली हमारे भाई-बन्दों के ही हाथों में हो- और उसका बहुत बड़ा हिस्सा है भी- तो हम उसका भी इसी तरह विरोध करेंगे। विदेश में तो कोई दूसरी क़ौम राज न करती थी, फिर भी रूस वालों ने उस हुकूमत को उखाड़ फेंका तो उसका कारण यही था कि जार प्रजा की परवाह न करता था।अमीर लोग मज़े उड़ाते थे, ग़रीबों को पीसा जाता था। यह बातें तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। वही हाल हमारा है। देश की सम्पत्ति किसी न किसी बहाने निकलती चली जाती है और हम ग़रीब होते जाते हैं।'
संपत्ति देश के बाहर जाए या देश में विभेद बना रहे, राष्ट्र की स्थापना व्यर्थ है।
‘कर्मभूमि’ उपन्यास में डॉक्टर शांति कुमार इसे थोड़े और विस्तार से यों कहते हैं,
..जब समाज का संचालन स्वार्थ-बुद्धि के हाथ में आ जाता है, न्याय बुद्धि गद्दी से उतार दी जाती है। ….समता जीवन का तत्त्व है। यही एक दशा है जो समाज को स्थिर रख सकती है। थोड़े से धनवानों को यह अधिकार नहीं है कि वे ईश्वरदत्त वायु और प्रकाश का अपहरण करें। यह विशाल जनसमूह अनधिकार, उसी अन्याय का रोषमय रुदन है।' प्रेमचंद नए समाज के गठन के रास्ते में बाधा संपत्ति को ही मानते हैं,
'संपत्ति ने मनुष्य को अपना क्रीतदास बना लिया है। उसकी सारी मानसिक, आत्मिक और दैहिक शक्ति केवल संपत्ति के संचय में बीत जाती है।..जब तक सम्पत्तिहीन समाज का संगठन न होगा, जब तक अस्म्पत्ति-व्यक्तिवाद का अंत न होगा, संसार को शान्ति न मिलेगी।' यह लेख कार्ल मार्क्स और गाँधी की याद दिलाता है जो निजी संपत्ति को ही मूल मानते हैं प्रत्येक प्रकार की संकीर्णता और हिंसा का।
समष्टि के लिए परिश्रम
पूँजीवाद को ख़त्म होना चाहिए सिर्फ श्रमिकों की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वह पूँजीपतियों को भी एक अमानवीय स्थिति की बाध्यता से मुक्त करता है। प्रेमचंद कुछ-कुछ मार्क्स और गांधी की तरह पूँजीपतियों को एक नई ज़िंदगी का न्योता देते हैं,
'...शांत मन से देखा जाए तो असम्पत्तिवाद की शरण में आकर उन्हें भी वह शांति और विश्राम प्राप्त होगा, जिसके लिए वे संतों और संन्यासियों की सेवा किया करते हैं।...अगर वे पिछले कारनामों को याद करें तो उन्हें मालूम हो कि संपत्ति जमा करने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा का, अपने सम्मान का, अपने सिद्धांत का कितना खून किया।..क्या वे अपने ही भाइयों,अपनी ही स्त्री से सशंक नहीं रहते? क्या वे अपनी ही छाया से चौंक नहीं पड़ते?' 'क्या ऐसे समाज में रहना उनके लिए असह्य होगा, जहाँ उनका कोई शत्रु न होगा, जहाँ उन्हें किसी के सामने नाक रगड़ने की ज़रूरत न होगी, जहाँ छल-कपट के व्यवहार से मुक्ति होगी।.. क्या वे उस विश्वास, प्रेम और सहयोग के संसार से इतना घबराते हैं, जहाँ वे निर्द्वंद्व और निश्चिंत, समष्टि के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करेंगे?'
इस आदर्श के ख़िलाफ़ यह तर्क स्वाभाविक मालूम पड़ता है कि बिना निजी स्वार्थ के कुछ भी करने के लिए प्रेरक शक्ति कहाँ से आएगी। प्रेमचंद का उत्तर सरल है, इतना कि उस पर अमल न किया जा सके यह कोई कह ही नहीं सकता:
'क्या गोसाईं तुलसीदास ने रामायण इसलिए लिखा था कि उसपर उन्हें रायल्टी मिलेगी। आज भी हम हज़ारों आदमियों को देखते हैं, जो उपदेशक हैं, कवि हैं, शिक्षक हैं, केवल इसलिए कि उन्हें मानसिक संतोष मिलता है।..
यह खुद ब खुद न होगा: 'क्या समष्टि के लिए परिश्रम करने में कष्ट होगा?'
प्रेमचंद जब निजी संपत्ति पर टिकी स्वार्थमय व्यवस्था के अंत की बात करते हैं तो वे ‘लाल क्रांति’ के पक्ष में नहीं हैं।
बोल्शेविक उसूलों का कायल हो चला हूँ, वाले उनके बयान से बहुत सारे लोग आज तक उत्साहित हैं। लेकिन वे किसी भी किस्म की तानाशाही के समर्थक भी नहीं हैं, वह सर्वहारा की तानाशाही ही क्यों हो।‘समाजवाद का आतंक’ शीर्षक छोटी सी टिप्पणी में वे व्यंग्यपूर्वक कहते हैं कि 'यह डिक्टेटरशिप का युग है। जनमतवाद के दिन लद गए।'
एक दूसरी टिप्पणी ‘मजूरदल का डिक्टेटरशिप से विरोध’ में वे इस बहस को खोलते हैं,
'डिक्टेटरशिप की कुछ चर्चा इंग्लैण्ड में भी होने लगी है।..मगर मजूरदल ने एक सभा करके डिक्टेटरशिप का विरोध किया है और जनतंत्र में अपने विश्वास की घोषणा की है।' समस्या यह है कि 'डिक्टेटरशिप कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है,यह सभी जानते हैं, मगर जब जनतंत्र केवल धनवानों और पूँजीपतियों के हाथ का खिलौना हो जाए, तो ऐसी दशा में स्वभावतः यह ख्याल होता है कि इस ढोंग से क्या फायदा। रूस, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, आस्ट्रिया, इटली, टर्की आदि देशों ने विवश होकर डिक्टेटरशिप की शरण ली, मगर इसमें कई दोष हैं। आज जो प्रजाहित का पुजारी है, संभव है कल वह स्वार्थ का पुजारी हो जाए, जिसकी मिसाल नेपोलियन है। फिर क्या ख़बर है कि एक डिक्टेटर के बाद दूसरा डिक्टेटर किस ढंग का आदमी हो।' जनतंत्र का अपहरण
इसके पहले प्रकाशित एक टिप्पणी से भ्रम हो सकता है कि वे ‘डिमोक्रेसी’ के आलोचक हैं। यह टिप्पणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई एक बहस की रिपोर्ट है। ‘डिमोक्रेसी’ की सीमा है और उससे सजग रहना ज़रूरी है:
‘डिमोक्रेसी’ केवल एक दलबंदी होकर रह गयी। जिनके पास धन था,जिनकी जुबान में जादू था, जो जनता को सब्जबाग़ दिखा सकते थे, उन्होंने डिमोक्रेसी की आड़ में सारी शक्ति अपने हाथ में कर ली। व्यवसायवाद और साम्राज्यवाद उस सामूहिक स्वार्थपरता के भयंकर रूप थे, जिन्होंने संसार को ग़ुलाम बना डाला और निर्बल राष्ट्रों को लूट कर अपना घर भरा।..' जिनके जुबान में जादू है उसे लफ्फाज भी कह सकते हैं। यह बात बहुत बाद में भारत की पहली माध्यमिक शिक्षा की रिपोर्ट लिखते हुए प्रोफ़ेसर मुदलियार ने दूसरे ढंग से कही जब उन्होंने लफ्फाजों द्वारा जनतंत्र के अपहरण की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि भाषा की शिक्षा में बहुत सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि जनतंत्र में भाषा, जुबान के जरिए जन का संगठन किया जा सकता है। इसका खतरा हमेशा रहता है कि लफ्फाजी करके कोई मजमेबाज जनता को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर ले। इसलिए भाषा की शिक्षा सच और झूठ के फर्क की तमीज़ दे सके जिससे भूसा और दाना अलग किया जा सके। प्रेमचंद हिटलर का उदय देख रहे थे।
इसलिए राष्ट्र बन रहा हो तो स्वार्थ के इस संगठन के प्रति सावधान रहने की ज़रुरत और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जनतंत्र के सहारे उसपर ताक़तवर कब्जा कर ले सकते हैं।
अगर राष्ट्र-राज्य बन रहा है तो हमेशा इसकी जाँच करते रहनी होगी कि वह किसी एक को अधिक अधिकार तो नहीं दे रहा,
'आज बीसवीं सदी में विशेष अधिकारों और स्वत्वों के राग अलापने का समय नहीं रहा।'
विशेष अधिकार खुद को उस प्रदेश की मूल आबादी कहनेवाले लोगों के हों, धर्म विशेष के लोगों के हों जो खुद को दूसरों के मुकाबले गुण और संख्या में श्रेष्ठ मानते हैं, कबूल नहीं किए जा सकते। अन्याय और ज़बरदस्ती पर टिके रिश्तों को उलटकर ही आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है,
'आज का राज्य ऐसी विषमताओं का समर्थक नहीं। आज का राज्य वह संस्था है, जिसका आधार-स्तम्भ है समता। उसका अर्थ है, प्रजामात्र के लिए समान अवसर, समान सुविधा और समान सत्ता की व्यवस्था करना, और जो राज्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह बहुत दिन टिक नहीं सकता।' प्रेमचंद यह भी कह सकते थे कि जिस क्षण से राज्य इस सत्य से विमुख हो जाता है, उसी क्षण उसका पतन आरंभ हो जाता है।












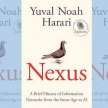













अपनी राय बतायें