पुलिस सुधार दिवस की 15वीं जयंति पर यह सवाल उठता है कि 22 सितंबर 2006 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अब तक क्यों लागू नहीं किया गया है? पुलिस को अधिक कुशल, बाहरी दबावों से मुक्त और जनता की ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए किए जाने वाले सुधारों के रास्ते में क्या अड़चनें हैं?
सर्वोच्च न्यायालय ने पहला निर्देश यह दिया था कि पुलिस प्रमुख का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार सबसे वरिष्ठ तीन पुलिस अफ़सरों की सूची से ही किया जाए। दूसरा निर्देश यह था कि ऑपरेशनल पदों पर तैनात पुलिस अफ़सरों के पद पर बने रहने की मियाद तय की जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस इस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के गठन का भी आदेश दिया था जिसमें पुलिस महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हों और इन्हें डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट (डीएसपी) से नीचे के रैंक पर नियुक्ति करने का अधिकार हो। इससे पुलिस में स्वायत्तता बढ़ेगी।
राज्य सुरक्षा आयोग
जनता की पुलिस का गठन करने के मक़सद से राज्य सुरक्षा आयोग बनाने की कल्पना की गई थी। इस आयोग के प्रमुख के रूप में गृह मंत्री, इसके सदस्य के रूप में विपक्ष के नेता, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व दूसरे लोग होंगे, जो पुलिस के कामकाज पर नज़र रखेंगे।
एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करने की बात भी थी, जो ज़िला व राज्य के स्तर पर होता। और अंत में, पुलिस को अधिक पेशेवर बनाने के लिए मामलों की जाँच और क़ानून व्यवस्था के कामकाज को अलग कर दिया जाता और अलग-अलग पुलिस अफ़सर ये काम करते।
ये सुधार पहले परीक्षण में ही लड़खड़ा गए।
कोई मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक चुनने का अधिकार अपने हाथ से नहीं जाने देगा। वह अपने वफ़ादार को उस पद पर बैठाना चाहेगा। मुख्यमंत्रियों का कहना है कि यह तो उनका अधिकार है, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है।
वरिष्ठ पुलिस अफ़सरों का कार्यकाल निश्चित करना राजनेताओं, अफसरशाही और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद है, क्योंकि उससे उन्हें अपनी ताक़त दिखाने का मौका नहीं मिलेगा।
पीईबी का विरोध
पीईबी का भी विरोध हुआ, क्योंकि राजनेता अनौपचारिक आदेश देकर पुलिस अफ़सरों का ट्रांसफर करवा लेते हैं। एक राज्य में तो ऐसा हुआ कि कुछ विधायकों के द्वारा थाना प्रभारी बनाने की एक सूची को नोट शीट पर दर्ज किया गया, लेकिन कुछ दूसरे विधायकों ने उसे रद्द कर एक दूसरी सूची उसी नोट शीट पर दर्ज कर दी।
राज्य सुरक्षा आयोग गठित किए जाने से पुलिस अफ़सरों को राजनीतिक दबावों से कुछ राहत मिलती, पर किसी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। और यही हश्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण का हुआ, जिसकी भूमिका सलाह देने तक सीमित थी।
सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक निर्देश का पालन हुआ है और वह है जाँच और क़ानून व्यवस्था के कामकाज को अलग करना। इसकी वजह यह है कि इससे राजनेताओं व अफ़सरशाही को सीधा नुक़सान नहीं है।
मॉडल पुलिस एक्ट
मानव संसाधनों की कमी की वजह से इसमें काफी रुकावटें आ रही हैं। नियंत्रक व महालेखाकार (सीएजी) ने हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि दिल्ली पुलिस के पास भी कम लोग हैं। यह हाल राजधानी का है।
और इस तरह पुलिस सुधार गृह मंत्रालय के फ़ाइलों के ढेर के नीचे दबा हुआ है। सुधार की प्रगति की जाँच कर रहे जस्टिस के. टी. थॉमस सुधार प्रक्रिया से बच निकलने के लिए राज्यों के किए गए सरल व अनूठे उपायों से भौंचक रह गए थे। राज्य अदालत के निर्देशों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कार्यकारी आदेश पारित करते जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट निरुपाय होकर देख रहा है।
सरकार मॉडल पुलिस एक्ट 2006 को लागू कर सकती थी। इसे सोली सोराबजी, कई पुलिस व आईएएस अधिकारियों, ग़ैरसरकारी सगंठनों और दूसरे लोगों ने मिल कर तैयार किया था।

नेशनल पुलिस आयोग
इसके अलावा जूलियो रीबेरो, के. पद्मनाभैया और वी. एस. मालीमथ जैसी हस्तियों की तैयार की हुई रिपोर्टें भी उपेक्षित पड़ी हुई हैं। साल 1977 से नेशनल पुलिस आयोग अभिलेखागार में उपेक्षित पड़ा हुआ था, इसमें दिए गए सुझावों को इनमें शामिल किया गया था।
क्या कोई उम्मीद है? मुख्यमंत्रियों से यह उम्मीद करना अव्यावहारिक है कि वे पुलिस को एक सीमा से अधिक स्वायत्तता देंगे। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस किसी मेयर या चुनी हुई सरकार के नीचे काम करती है।
हमारे यहाँ जहाँ ज़मीनी स्तर की राजनीति थानों, कचहरियों और तहसीलों के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है, यह सोचना मुश्किल है कि पुलिस राजनीतिक दवाबों से पूरी तरह मुक्त हो।
राजनीतिक रुझान
लेकिन सुधार सिर्फ कार्य अवधि और स्वायत्तता तक सीमित नहीं है। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रमुख का कार्यकाल दो साल तय होने के बावजूद कई मामलों में इस संगठन के कामकाज में राजनीतिक रुझान साफ दिखा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को नियम क़ानून मान कर चलने वाला और जनता के प्रति ज़िम्मेदार होना चाहिए।
प्रधानमंत्री के कुशल व स्मार्ट पुलिस के विज़न को पूरा करने के लिए सभी राज्यों के आईपीएस नेतृत्व को सिस्टम के अंदर ही सुधार का बिगुल फूंक देना चाहिए।
- सबसे पहले, पुलिस को यूएपीए यानी अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ प्रीवेन्शन एक्ट और राजद्रोह क़ानूनों का दुरुपयोग एकदम रोक देना चाहिए।
- दूसरे, पुलिस को सांप्रदायिक या जातिगत पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए।
- तीसरे, महिलाओं के प्रति अपराध से निपटने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- चौथे, इस डिजिटल युग में प्रक्रिया तेज़ करनी चाहिए और जनता से जुड़ाव बढ़ाना चाहिए।
- और अंत में, बेकाम हो चुके और ग़ैरक़ानूनी काम करने वाले तत्वों से सख़्ती से निपटना चाहिए।
जनता की भागीदारी
जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, पुलिस महानिदेशकों को चाहिए कि वे अपने सालाना सम्मेलनों का एजेंडा साहसिक और उद्देश्यपूर्ण रखें। इसमें आम जनता की भी भागीदारी हो। पुलिस विशेषज्ञता अंदरूनी मामला हो सकता है, पर इसका नतीजा सबको दिखना चाहिए।
संस्था के रूप में गृह मंत्रालय नए किस्म के पुलिस प्रशासन के लिहाज से पुराना और अप्रासंगिक हो चुका है और यह खुद को बदल नहीं सकता। आंतरिक मंत्रालय का कामकाज बदल दिया जाना चाहिए, उसे पेशेवर लोग चलाएं और उस पर सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री का नियंत्रण हो।
पुलिस में व्यापक सुधार के लिए यह भी ज़रूरी है कि कॉरपोरेट जगत, उद्योगपतियों, आईआईटी, विश्वविद्यालयों, ग़ैरसरकारी संगठनों, रिटायर्ड पेशेवर लोगों, स्टार्ट अप वगैरह की मदद ली जाए।
इनकी मदद से ऑनलाइन अपराध पर नज़र रखी जा सकती है, आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेन्स, प्रशिक्षण, आधुनिक हथियार वगैरह की व्यवस्था की जा सकती है।
कुछ सांसदों के दिए संकेत स्वागतयोग्य हैं, उन्होंने निगरानी सुधार और खुफ़िया एजेन्सियों के लिए ओवरसाइट कमेटियों की बात कही है।
इसी तरह थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी, ग़ैरसरकारी संगठन और अकादमिक जगत के लोगों को व्यापक पुलिस सुधार का समर्थन करना चाहिए।
मॉडल पुलिस एक्ट 2006 को लागू करने का एकदम सही समय आ गया है, ताकि नए भारत के विज़न के साथ पुलिस प्रणाली कदम से कदम मिला कर चल सके।

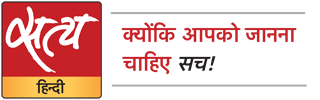






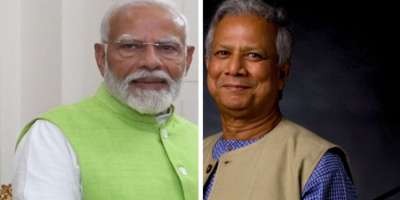














अपनी राय बतायें