सवाल - लॉकडाउन कैसा गुजरा?
जवाब -सच्ची, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे घर पर रहने की आदत है। मैं फ़िल्में करता हूँ, जो ज़्यादातर एक ही दौर में ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद मैं एकाध महीने की छुट्टी ज़रूर लेता हूँ। अपने घर पर पड़ा रहता हूँ, बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, फ़िल्में देखता हूँ, टेनिस खेलता हूँ, अपने फार्म हाउस पर चला जाता हू। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले तो मुझे ये ख्याल आया कि थिएटर तो बंद हो गया। थिएटर मेरी नसों में ख़ून की तरह बह रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे कमी उसकी महसूस हुई। हॉर्न की आवाजें नहीं सुनाई दे रही थीं, ट्रैफिक जाम नहीं लग रहे थे, लोग एक-दूसरे का लिहाज रख रहे थे। एकाध बार तो ऐसा हुआ कि जब टहलते हुए जेब्रा कॉसिंग पर एक गाड़ी मेरे लिए रुकी, जो कि कभी नहीं होता है। लोग नहीं रुकते यहां पर क्योंकि ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। और आसमान साफ था, समुद्र नीला नजर आने लगा, मछलियां, जानवर, पक्षी, वह तो सब हुआ ही। लेकिन घर में बंद रहने से मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, जितनी थिएटर में काम न करने की वजह से। हमेशा इससे ही अपना दिमागी तवाजुन थिएटर के सहारे ही संभाला है।
एक ऐसा दौर था, जब मैं कई सारी फ़िल्में कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि सब उसे भूल गए हैं अब, सब एक से एक बेहूदा फ़िल्में थीं। पैसा बहुत कमा रहा था और परेशानी हो रही थी कि क्या मुझे जिंदगी भर इसी तरह की फ़िल्में करनी पड़ेंगी? मैं तो इससे बावला हो जाऊँगा। थिएटर ही था जिसने मुझे बचाया। उस दौरान में मैं दिन में शूटिंग करता था और शाम को पृथ्वी थिएटर में आकर शो करता था। नौजवान था उस वक़्त, 30-32 साल की उम्र थी, स्टेमिना बहुत था, मगर अब मुझसे वो नहीं हो पाएगा।
लेकिन थिएटर का मुझपर बहुत बड़ा कर्ज है, जो मैं चुका नहीं पाऊँगा। जो कुछ भी मैंने सीखा है और पाया है, वह थिएटर से ही पाया है और इससे मेरा जुड़ाव कभी खत्म नहीं हो सकता, भले ही फ़िल्मों से मेरा जुड़ाव ख़त्म हो जाए। तो इस दौरान एक तो मैंने घर में झाड़ू और पोंछा लगाना सीखा, जो कि कभी नहीं किया था। किचन में जाकर मदद किया करता था। रत्ना हालाँकि मुझे भगा देती थीं। फिर भी प्याज, आलू, टमाटर वगैरह काटा करता था। एकाध बार दाल भी बनाई तो मुझे बड़े अचीवमेंट का अहसास हुआ। और ये आदत मैंने अब बना ली है कि मुझे घर में कुछ न कुछ मदद करनी है और ये मुझे बहुत पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। घर में हमारे कोई भी टेंशन नहीं। न डोमेस्टिकली, न बच्चों के साथ। रमजान का महीना भी चल रहा था तो एक महीना तो यूँ ही निकल गया, इफ्तारी के इंतज़ार में। सुनने में आया कि जेहनी बीमारियाँ बहुत फैल रही थीं लॉकडाउन के दौरान, डोमेस्टिक वॉयलेंस बहुत हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही थी, सेपरेशन बहुत हो रहे थे। जितना मैं सोच रहा था कि इतनी फ़िल्में देखूँगा, मगर पहले हफ्ते तो टीवी खुला ही नहीं। क्योंकि रत्ना, मैं और मेरे बेटे ने सोचा कि हम शेक्सपीयर पढ़ते हैं। जब तक मेरा बेटा झेल पाया, हमने बैठकर पढ़े। फिर वो अपने काम में लग गया। लेकिन मैंने शेक्सपीयर साहब के सारे नाटक पढ़ डाले। क्योंकि मुझे ख्याल आया कि जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ़ वेनिस ये तो हर कोई जानता है। लोगों को ये भी मालूम है कि मैक्बेथ और हेमलेट क्या है, हालाँकि लोग उनकी कहानियों में कन्फ्यूज होते हैं। मैंने सात या आठ नाटक उनके पढ़े थे, तीन चार में काम किया था। और दो तीन ऐसे थे, जिनके बारे में सरसरी तौर पर मालूम था। मैंने सोचा कि पैंतीस नाटक लिखे हैं इस शख्स ने। और मैंने कुल बारह से वाकफियत है मेरी।
मैंने बैठकर पूरे पढ़ डाले। सब बहुत अच्छे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। कुछ उसमें बहुत ही बेहूदा हैं। हैरत होती है कि ये कैसे लिख दिया शेक्सपीयर साहब ने।
लेकिन उनको पढ़कर मेरा ये बीलीफ और भी पुख्ता हो गया कि हिंदी सिनेमा का कोई भी फ़ॉर्मूला ना होता, अगर शेक्सपीयर ना होता। सारे के सारे हिंदी सिनेमा के क्लीशेज शेक्सपीयर से उधार लिए हुए हैं। फैज साहब के बारे में एक नाटक की तैयारी शुरू की ऑनलाइन। ज़ूम में हम लोग रिहर्सल किया करते थे। फैज साहब की कैद का जो दौर था, जिसमें उन्हें रावलपिंडी कॉन्सिपिरेसी में बंद कर दिया था। इस बहाने उनकी कुछ और शायरी भी पढ़ ली। ये नाटक धीरे धीरे तैयार हो रहा है, देखिए कब पेश कर पाएंगे। लॉकडाउन खुल जाने के बाद सबसे ज्यादा खुशी यह थी कि पृथ्वी थिएटर खुला। हालाँकि दो सौ की जगह सौ लोग बैठते हैं। मगर उस रंगमंच पर वापस जाकर जो खुशी मिली, वह मैं बयान नहीं कर सकता।
सवाल - कोरोना से पहले और बाद की दुनिया में क्या फर्क दिख रहा है?
जवाब -
पहले तो ये कि मुझे उम्मीदें क्या थीं, वो मैं बता दूँ। एक तो अगर आप आज के दौर में ये भी कह दें कि हम हिंदुस्तानी ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करते तो आपको एंटीनेशनल बना दिया जाएगा। अगर ये कह दें कि हम हिंदुस्तानी एक दूसरे का लिहाज नहीं करते या फिर हिंदी फ़िल्में मुझे पसंद नहीं है तो आप गद्दार करार दिए जाएंगे, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि शायद कहीं पर एक भाईचारे जैसी फीलिंग आए, जो कि 26-11 के बाद आपको याद हो, जब उन कमबख्तों ने हमला किया, बहुत से लोगों को मारा, खुद भी मरे, उस पर अफसोस तो है ही, लेकिन उस वक़्त किसी को मजहबी फर्क का ख्याल भी नहीं आया। कितने मुसलमान भी मरे, उन मुसलमान कमबख्तों ने मारा। हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को भी, सबको मारा, बेरहमी से मारा, बिना भेद किए मारा। मुझे लगा कि इन लोगों ने हम पर एक फेवर कर दिया है कि हम सब मिलकर इस खबीस बिहेवियर का सामना कर पाएंगे, अफसोस कि ऐसा अगले सालों में हुआ नहीं, बल्कि डिविजंस और भी बढ़ गए।
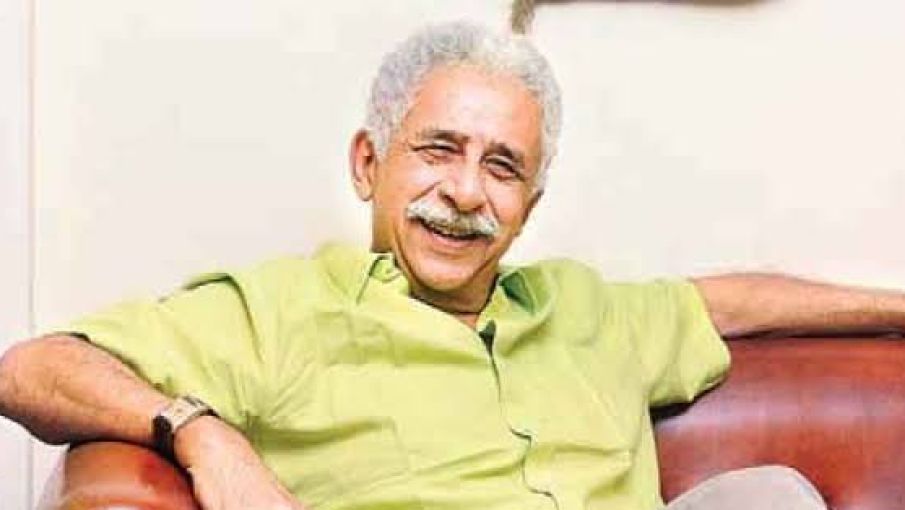
कोविड के दौरान चार घंटे का नोटिस देकर जो लॉकडाउन अनाउंस किया गया, नहीं मालूम कि वो जायज था या नहीं, उस पर मुख्तलिफ रायें हैं, लेकिन शाहीन बाग़ के प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए वो ज़रूर एक बहुत बढ़िया चाल थी, और जो कि हो गया। अब ये बर्ड फ्लू फैला है, तो किसानों के आंदोलन को तितर बितर करने के लिए मेरे ख्याल से ये सरकार के बहुत काम आएगा। उम्मीद थी कि लिहाज बढ़ जाएगा एक दूसरे के लिए। जब फ्लाइटें उड़ना शुरू हुईं तो लोग दूर खड़े रहते थे, कहना मानते थे। वो तो सब वैसे ही गायब हो गया। लोग हॉर्न मारते रहते हैं, हवाई जहाज से उतरते हैं तो ऐसे भागते हैं कि दूसरी फ्लाइट पकड़नी होगी। ये तो अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दुनिया कितनी बदली है, वो तो ऑनलाइन हो गई है सारी दुनिया, और मेरे ख्याल से अब ये रवैया बन जाएगा। शायद दफ्तर जाना इतना लाजिम ना हो, जितना पहले था। ड्रामे भी ऑनलाइन होने लगे हैं, फ़िल्में तो ऑनलाइन देखते ही रहे हैं। तो कहीं पर ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें मेरे ख्याल से काफी कुछ बदलेगा। बेहतरी के लिए या बदतरी के लिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बदलेगा बहुत।
सवाल - दुनिया के अलावा खुद में क्या फर्क पा रहे हैं?
जवाब -
मैं खुद में शायद ये फर्क पा रहा हूँ कि जब्त थोड़ा ज्यादा आ गया है। गुस्से का तो मेरे बहुत लोगों ने जिक्र किया है। वो एक आदत सी थी, जिसमें मैं बचपन से पड़ गया था। उस आदत को इस दौरान मैं तोड़ पाया हूं। खानदानी रिश्ते और गहरे हो गए हैं। एक साल से मेरी मेरे भाइयों-भाभियों से मुलाक़ात नहीं हो पाई, विदेशों में दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाक़ात नहीं हो पाई, सिर्फ़ बात हो पाई। कहीं पर वो एब्सेंस मेक्स द हार्ट क्रो फाउंडर वाली जो बात है, वो हो गई है कि हम शायद ज्यादा एप्रीशिएट कर सकेंगे एक दूसरे की दोस्ती, मोहब्बत को, ख्यालों को, लिहाज को।
सवाल - हमने आपकी जवानी देखी, अब बुढ़ापा देख रहे हैं। आप बहुत कुछ कह चुके हैं। अब भी कुछ बचा है कहने को?
जवाब -
कहने के लिए तब तक कुछ न कुछ बाकी रहेगा, जब तक दिल में कोई न कोई टीस उठती है। लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट्स की तसवीरें देखकर मेरा दिल टूटता था। इनके ऊपर जो पुलिस की ज्यादितयां हो रही थीं, बहुत हैरत और अफसोस होता था यह देखकर कि ये पुलिसवाले जो उन लोगों को डंडे मार मार कर भगा रहे हैं, ये भी तो उसी तबक़े के हैं। जरा सा हालात में बदलाव से हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ये भी होते सड़क पर और कोई इन्हें डंडे मार रहा होता, मेरा दिल बहुत दुखता था। फ़िल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है कि 65 साल की उम्र हो तो आप काम नहीं कर सकते। ये क्या अहमकाना रूल है कि आप 64 के हों तो ठीक है, मगर 65 के हों तो नहीं चलेगा। जबकि कितने जवान एक्टरों को कोविड हुआ है। और फिर एक्टिंग में तो बूढ़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। चाहे आप नौजवान लड़के-लड़की की स्टोरी बना रहे हो, तो आपको उनके मां बाप तो चाहिए ही, या प्रिंसिपल तो चाहिए ही। तो बुजुर्ग एक्टरों को एकॉमडेट करना था उन्हें, सो उन्होंने कर दिया। लेकिन फर्क उन्हें पड़ेगा, जो 65 साल का लाइट बॉय है, कैमरा अटेंडेंट, या जो यूनिट को चाय पिलाता है, जो मेकअप करते हैं, एक्स्ट्रा हैं, स्टंटमैन हैं, डांसर हैं, इनमें से कोई 65 साल से ऊपर हुआ तो? मेरी, परेश रावल या बच्चन साहब की बात और है, उन्हें तो कोई भी ले लेगा, इन लोगों को तो फौरन हटा दिया जाएगा। मुझे बहुत चुभती है ये बात और नाइंसाफी लगती है। नहीं पता कि रसोई में जो काम करते थे, उनका क्या हुआ होगा। दुआ करता हूं कि इस तबक़े की मेहनत को, योगदान को शायद अब पहचाना जाए।
सवाल - एक तबक़ा है, जो समझता सबकुछ है, मगर बोलता कुछ नहीं। फिर एक तबक़ा है जो बोलता बहुत है, पर समझता नहीं। ऐसे में जो चुप हैं, वे क्या करें?
जवाब -
ये आपके जमीर की बात है। आप किसी को उकसा तो नहीं सकते कि इसमें यकीन करो। अगर आपका जमीर चुभता है तो उन्हें कहना चाहिए। और ये बहुत ही मशहूर बात है कि जब सब कुछ तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर उतना परेशान नहीं करेगा, जितनी आपको आपने दोस्तों की खामोशी चुभेगी। मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर किसान वहाँ जमीन पर कड़कती सर्दी में बैठे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा- ये हम नहीं कह सकते अब। मुझे उम्मीद है कि किसानों का प्रदर्शन फैलेगा और आम जनता इसमें शामिल होगी। खामोश रहना जुल्म करने वाले की तरफदारी करना है, ऐसा मानता हूं। और हमारे बड़े बड़े धुरंधर लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग चुप बैठे हैं। इसलिए कि उनको लगता है कि बहुत कुछ खो सकते हैं वो। अरे भई, जब आपने इतना कमा लिया कि आपकी सात पुश्तें बैठ कर खा सकती हैं तो कितना खो लोगे आप?
सवाल - क्या दुनिया का और अपना भी वही मुस्तकबिल दिखता है, जो सोचा था? या अभी यह सोच से भी बुरा दिखता है या उम्मीद से अच्छा?
जवाब -
जो हो रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि, और मुश्किल यह है कि किसी भी तरह के ख्यालों के एक्सचेंज की गुंजाइश ही नहीं रही। अगर आप कुछ भी कहें तो फौरन आप पर कुछ न कुछ इल्जाम लगाया जाएगा। एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि एक इंसान (पुलिसवाले) की मौत एक गाय की मौत से कम अहमियत लगती है। जो उधम मचा, मुझे नहीं पता क्यों मचा था। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा कि एक इंसान की मौत कम अहमियत रखती है, तो इसका इंटरप्रिटेशन किया गया कि मुझे डर लग रहा है। मैंने बार बार दोहराया कि मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अपने मुल्क में हूँ, तीन सौ साल से मेरी पुश्तें यहाँ पर हैं, अगर ये भी चीजें मुझे हिंदुस्तानी नहीं बनातीं तो कौन सी चीजें किसी को हिंदुस्तानी बनाती हैं? अब लव जिहाद लेकर आए हैं कि हिंदू मुसलमान में रिश्ते का तो सोचें ही ना, आपस में मिलना जुलना भी छोड़ दें। जब हमारी शादी होने वाली थी, तब मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा, कि क्या तुम रत्ना का ईमान लाओगे तो मैंने मना कर दिया। मेरी अम्मी बोलीं, हां, सही है। मजहब कैसे बदल सकते हो। जो बातें बचपन में सिखाई गई हैं, उन्हें आप कैसे बदल सकते हैं। ये मेरी अम्मी का कहना था, जबकि वे बेहद ऑर्थोडॉक्स फैमिली की थीं।
सवाल - लोकतंत्र पर कुछ कहेंगे, अगर बुरा न लगे?
जवाब -
एक अंग्रेजी की कहावत है कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट, एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। और दुनिया की जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, यानी अमेरिका, वहां डेमोक्रेसी का क्या हश्र हो रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। मेरे लिए डेमोक्रेसी का डेफिनेशन यह है कि सबके बराबर हक तो हों, पर सबकी बराबर ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए। एक सेंस ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हममें पैदा नहीं होगी कि मैं दूसरे का थोड़ा ख्याल रखूँ। अगर कोई गाड़ी आगे ले कर जा रहा है तो उसे अहम का सवाल न बनाएँ। जब तक डंडा लेकर कोई बैठा ना हो, तब तक हम अपना फर्ज पूरा नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेसी का आइडियल नहीं है। हमें बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। जो कहीं नहीं हुआ, बल्कि कम्युनिज़्म में भी नहीं हुआ। वहाँ भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। तो बराबरी की ज़िम्मेदारी हर एक को लेनी होगी।
(जमील गुलरेज़ एडवरटाइज़िंग और रंगमंच की मशहूर हस्ती हैं। कथाकथन नाम से भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं।)































अपनी राय बतायें